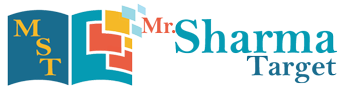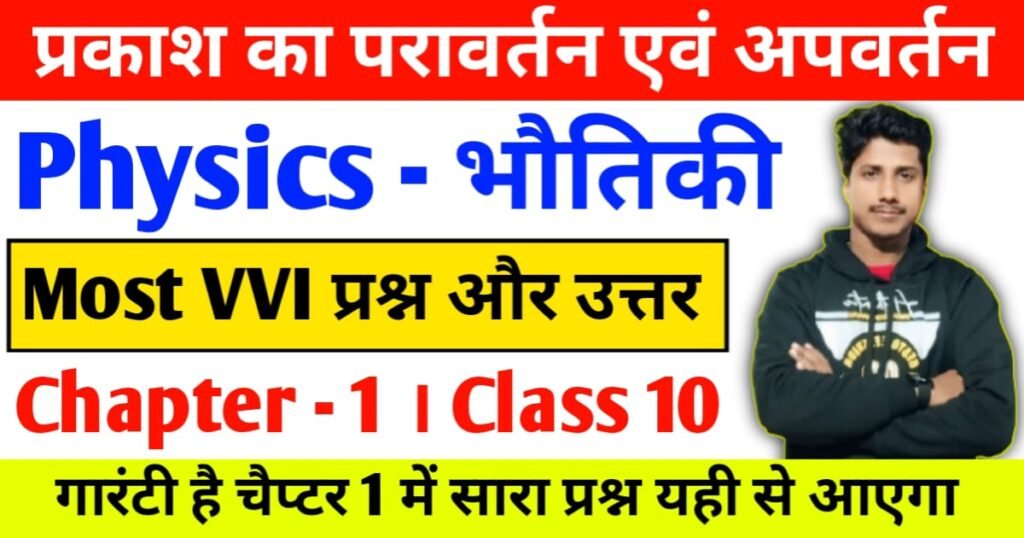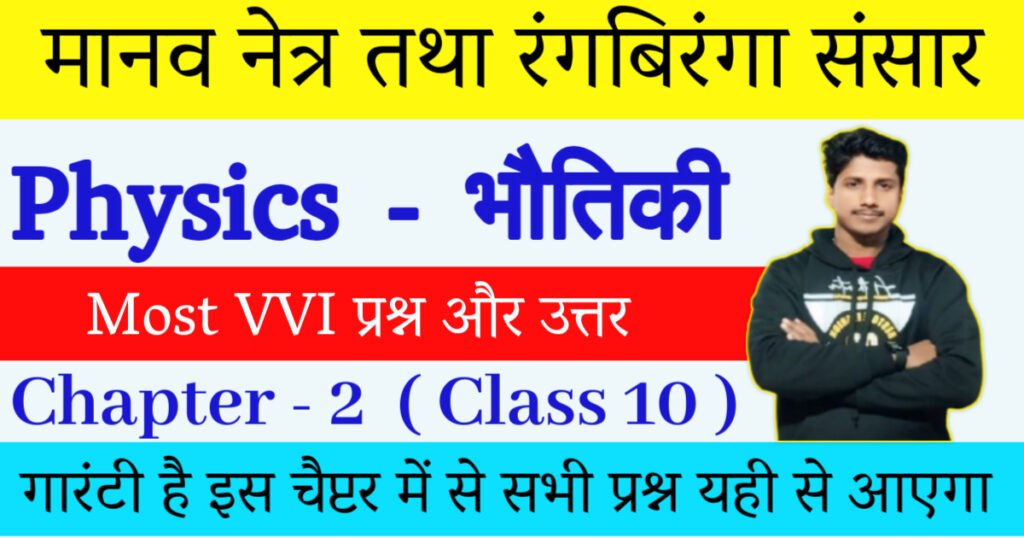Bihar Board Class 10th Science Model Paper 2026 Set – 2
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 विज्ञान मॉडल सेट – 2 में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर के साथ अच्छे से डिस्कशन किया गया है। यदि आप मैट्रिक परीक्षा 2026 में विज्ञान में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस पोस्ट में दिए गए सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अच्छे से कमांड कर लीजिए। गारंटी है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में सभी प्रश्न यहीं से आएंगे।
| Subject | Science ( Model Paper ) |
|---|---|
| Class | 10th |
| Model Set | 2 |
| Session | 2025-26 |
| Subjective Question | All Most VVI Questions |
Physics – भौतिकी | Model Set – 2 | Class 10 | By-Suraj Sir
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही चार प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए दो अंक निर्धारित है।
1. विद्युत फ्यूज क्या है ? यह किस मिश्र धातु का बना होता है ?
Ans- विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है। अतिभारण एवं लघुपथन से परिपथ की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
- ताँबे तथा टिन अथवा शीशा एवं टिन के मिश्रधातु के तार का उपयोग किया जाता है।
2. रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है ?
Ans- रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अन्यों रंगों की तुलना में सर्वाधिक होने के कारण लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। जिसके कारण धुँध या घना कोहरा में भी लाल रंग साफ-साफ दिखाई देता है।
3. विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं ?
Ans- किसी चालक को किसी परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युतवाहक बल उत्पन्न होने को वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं।
4. प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें।
Ans- प्रकाश का परावर्तन एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें किसी एक माध्यम में चलता प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश का इस तरह परावर्तित होना कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है जिन्हें प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं।
- परावर्तन के नियम के दो नियम है-
(i) आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक तल पर आपतन बिन्दु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं।
(ii) आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है।
ये नियम ही प्रकाश के नियम कहे जाते हैं।
5. विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्तरीयों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं ?
Ans- मिश्रधातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। उच्च ताप पर भी ये मिश्रधातु ऑक्सीकृत नहीं होते। इसी कारण टोस्टर, इस्तरी आदि विद्युत तापन युक्तियों के चालक शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्रधातु के बनाए जाते हैं।
6. किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नील की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है ?
Ans- अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊँचाई पर होते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता और न ही यहाँ कोई प्रकीर्णन हो पाता है इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है।
7. अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है ?
Ans- अपवर्तनांक को परिभाषित – अपवर्तनांक एक माध्यम का वह गुण है जो यह बताता है कि प्रकाश उसे माध्यम में कितनी गति से चलता है। इसे n से सूचित किया जाता है।
हमें पता है कि हीरे का अपवर्तनांक ( 2.42 ) सबसे अधिक है। इसलिए इसका प्रकाशित घनत्व भी सबसे अधिक है।
जैसे- n=c/v ( जहां c निर्वात में प्रकाश की गति है तथा v माध्यम में प्रकाश की गति है। )
यदि n सबसे अधिक है तो v सबसे छोटा होगा। इसलिए हीरे के प्रकाश की गति सबसे कम है।
8. घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ?
Ans- श्रेणीक्रम संयोजन में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही परिपथ होता है। यदि ऐसे परिपथ में लगे उपकरणों में से कोई एक उपकरण खराब हो जाए तो परिपथे में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 09 एवं 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही एक का उत्तर दें।
9. प्रतिरोध और विभावांतर के S.I. मात्रक को लिखे। ओम के नियम को सत्यापन कर समझाएं।
Ans- प्रतिरोध एवं विभवांतर के S.I. मात्रक क्रमशः ओम ( Ω ) और वोल्ट ( V ) है।
- अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होनेवाली विद्युतधारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है।
प्रायोगिक सत्यापन: — एक आसान से प्रयोग की सहायता से ओम के नियमों को सत्यापित किया जा सकता है।
इसके लिए आवश्यक परिपथ को चित्र में दिखलाया गया है। कई सेलों को श्रेणीक्रम में जोड़कर एक बैट्री तैयार
की जाती है जिसके समानान्तर एक रियोस्टेट Rh लगाया हुआ है। यह पूरी व्यवस्था विभव पात के नाम से जानी जाती है,
जिससे मनचाहा विश्वा० बल मुख्य परिपथ पर आरोपित किया जा सकता है। इसके कारण बल्ब B तथा धारा नियंत्रक
प्रतिरोध R पर लगते विभवान्तर को मापने के लिए उनके समानान्तर एक वोल्टमीटर (V) भी लगा दिया जाता है।
परिपथ में लगा ऐमीटर प्रवाहित धारा (i) का मान बतलाता है। कुंजी K को बन्द करते परिपथ से धारा बहने लगती है।
जब रियोस्टेट के परिवर्तनशील टर्मिनल को A के निकट रखते हैं तो परिपथ पर लगता विभवान्तर छोटा होता है।
उसे जैसे-जैसे B की ओर खिसकाते हैं आरोपित विभवांतर का मान बढ़ता है और उसी के साथ प्रवाहित धारा भी बढ़ती जाती है। अलग-अलग विभवान्तर और संगत के धारा का मान क्रमशः वोल्मीटर तथा ऐमीटर से नोट कर लेते हैं। इस प्रकार रियोस्टेट की सहायता से V तथा I के कई जोड़े पठन प्राप्त कर लिये जाते हैं जिन्हें क्रमशः X तथा Y-अक्ष के अनु रखते हुए एक ग्राफ खींचा जाता है। पाया जाता है कि यह ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में मिलता है जो बतलाता है कि V ∝ I इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है।
10. विद्युत मोटर क्या है ? इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें।
Ans- विद्युत मोटर – विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह धारावाही चालक पर चुम्बकीय क्षेत्र में लगते बल के सिद्धांत पर काम करता है।
बनावट : इसके मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं-
आर्मेचर : एक नरम लोहे के कोर पर ताँबे के तार, जिनपर विद्युतरोधी पेन्ट चढ़ा होता है, को लपेटकर आर्मेचर बनाया जाता है।
दिपरिवर्तक : द्विपरिवर्तक का उपयोग कुण्डली में धारा की दिशा को प्रत्येक आधे चक्र के बाद पलटने के लिए किया जाता है। यह ताँबे का बना एक वलय होता है जो बीच से दो भागों C₁ तथा C₂ में बँटा होता है।
कार्बन व्रश : कार्बन के दो छोटे टुकंड़े, जो कार्बन ब्रश के नाम से जाने जाते हैं, परिवर्तक के विभक्त वलयों को सदा स्पर्श करते रहते हैं।
नाल चुम्वक : आर्मेचर एक प्रबल नाल चुम्बक के दोनों ध्रुवों के बीच घूमता है।
विद्युत मोटर की कार्य पद्धति : कार्बन ब्रशों से होकर जब आयताकार कुण्डली में धारा प्रवाहित होती है तो कुण्डली के आमने-सामने की भुजाओं में परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा का प्रवाह होता है जिससे चुम्बकीय क्षेत्र में वे कुण्डली के तल के लंबवत् पर विपरीत दिशा में बल का अनुभव करते हैं। 
इस तरह से बना बलयुग्म कुण्डली को अपने अक्ष पर घूर्णित कराता है। जब कुण्डली में 180° का घूर्णन पैदा हो जाता है तो उसकी दोनों भुजाओं का विनिमय हो जाता है जिससे C₁ तथा C₂ का संपर्क कार्बन ब्रशों से बदल जाता है। इस कारण अभी भी कुण्डली से N S धारा का प्रवाह पूर्व की तरह बना रहता है जिससे कुण्डली की घूर्णन गति पूर्व की तरह ही रहती है। इस प्रकार स्रोत से धारा मिलते रहने पर कुण्डली लगातार घूमती रहती है और उसकी धुरी से किसी यंत्र को जोड़कर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
Chemistry – रसायन विज्ञान | Model Set – 2 | Class 10 | By-Suraj Sir
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 11 से 17 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही चार प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए दो अंक निर्धारित है।
11. जब लोहे की किस को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है , तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है ?
Ans- लोहे की कील, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सलफेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलीन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है।
Fe(s) + CuSO4(aq) → FeSO4 (aq) + Cu(s)
12. निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए-
(a) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है।
(b) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है।
Ans- (a) Zn + H₂SO₄ → ZnSO4 + H2
(b) Mg + 2HСІ → MgCl2 + H2
13. निम्न पदों की परिभाषा दें – (i) खनिज (ii) भर्जन
Ans- (i) खनिज : खनिज वह पदार्थ है जिन्हें खानों से निकाला जाता है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली रहती है।
(ii) भर्जन : सान्द्रित अयस्क को अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित कर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना द्रवित गर्म करने की क्रिया भर्जन अथवा जारण कहलाती है। यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के साथ की जाती है।
14. उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ? एक उदाहरण दें।
Ans- द्वि-विस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षार के बीच होता है तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
HCI + NaOH → NaCl + H₂O
15. बेकिंग पाउडर क्या है ?
Ans- बेकिंग पाउडर बारीक सफेद पाउडर होता है जिसका खमीर पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर एक एसिड (तारतर का क्रीम) और खार (येकिंग सोडा) का मेल है।
16. बुटानोने एवं एथनिक अम्ल के संरचना सूत्र लिखें।
Ans- 
17. ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है ? उदाहरण दीजिए।
Ans- ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया : वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात् ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है।
CaO+H₂O → Ca(OH)2 + ऊष्मा
ऊष्माशोषी अभिक्रिया : वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के अवशोषण के बाद अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है।
2NH CI + Ba(OH)2 + ऊष्मा → BaCl2 + 2H2O + 2NH3
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 18 एवं 19 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही एक का उत्तर दें।
18. प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें।
Ans- प्रयोगशाला में मिथेन बनाने की विधि – प्रयोगशाला में सोडियम ऐसीटेट तथा सोडा लाइम (NaOH + CaO का मिश्रण) के मिश्रण को गर्म करके मिथेन गैस बनायी जाती है।
CH3COONa + NaOH गर्म → CH + Na₂CO3
क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया – मिथेन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के विसरित प्रकाश में रख देने पर मिथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। इसमें मिथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु बारी-बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है।
CH4 + Cl₂ → CH3CI + HCI ( क्लोरोमेथेन )
CH3CI + Cl₂ → CH₂Cl₂ + HCI ( मिथिलीन डाइक्लोराइड )
CH2Cl2 + Cl2 → CHCI3 + HCI ( क्लोरोफॉर्म )
CHCI3 + CI2 → CCI4 + HCI ( कार्बन टेट्राक्लोराइड )
19. मिश्रधातु किसे कहते हैं ? इसके दो उदाहरण दें। मिश्रधातु के तीन उपयोगी का वर्णन करें।
मिश्रधातु की परिभाषा – मिश्रधातु दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रधातु कहते हैं।
उदाहरण – (1) पीतल, ताँबा (Cu) एवं जस्ता (Zn) की मिश्रधातु है। (ii) काँसा, ताँवा (Cu) एवं टिन (Sn) की मिश्रधातु है।
मिश्रधातु के तीन उपयोग-
(1) इस्पात : इसका उपयोग रेल लाइन पुल, जहाजों, भवनों एवं यातायात के साधनों के निर्माण में।
(ii) पीतल : इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, मूर्ति, वाद्ययंत्र, मशीन के पार्टस, तार, वैज्ञानिक उपकरण, नट-वोल्ट, ताला, कारतूस, सिक्का बनाने में।
(iii) सोल्डर : लेड + टिन के मिश्रण से बनाये जाते हैं। इसका उपयोग बर्तन के जोड़ों में, टाँका लगाने में, विद्युत तारों की बेल्डिग में।
Biology – जीवविज्ञान | Model Set – 2 | Class 10 | By-Suraj Sir
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 20 से 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही चार प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए दो अंक निर्धारित है।
20. हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है ?
Ans- अमाशय के आंतरिक भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। इस रस का एक पटक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
भोजन के पाचन में HCI की भूमिका-
(i) यह टायलिन की क्रिया को रोक देता है।
(ii) यह भोजन को सड़ने से बचाता है।
(iii) यह भोजन के साथ आगे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है।
(iv) यह भोजन का माध्यम अम्लीय बना देता है ताकि उसपर जठर रस का एंजाइम जैसे पेप्सिन अभिक्रिया कर सके।
(v) यह निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदल देता है।
21. श्वसन श्वासोच्छ्वास से किस प्रकार भिन्न है ?
Ans- श्वसन श्वासोच्छ्वास से निम्नलिखित प्रकार भिन्न है-
श्वसन
(i) यह एक जैव रासायनिक प्रक्रम है।
(ii) इसमें कोशिका के भीतर संचति भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है।
(iii) यह कोशिका के भीतर माइटोकॉण्ड्रिया में संपन्न होता है।
(iv) इसमें ऊर्जा मुक्त होती है।
(v) इसमें एंजाइम भाग लेते हैं।
श्वासोच्छ्वास
(i)यह एक भौतिक (यांत्रिक)प्रक्रम है।
(ii) इसमें केवल गैसों का आदान-प्रदान होता है।
(iii) यह श्वसनतंत्र में संपन्न होताहै।
(iv) इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती है।
(v) इसमें एंजाइम भाग नहीं लेते हैं।
22. स्थानांतरण क्या है ? पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस प्रकार होता है
Ans- पौधों की पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ (स्टार्च) के रूप में तैयार करती है और वहाँ से निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में एक विलयन के रूप में भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद का संवहन स्थानांतरण कहलाता है।
स्थानांतरण की यह प्रक्रिया संवहन ऊतक के एक प्रकार फ्लोएम ऊतक द्वारा की जाती है। फ्लोएम ऊतक एक जटिल संवहन ऊतक है जिसमें चालनी नली, सखि कोशिकाएँ, फ्लोएम मृदुत्तक तथा फ्लोएम तंतु मौजूद होते हैं। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सभी दिशाओं में होता है।
23. शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है ? इसके दो प्रमुख कार्यों को लिखें।
Ans- शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क (kidney) है।
वृक्क के कार्य –
(i) रक्त से अपशिष्ट पदार्थ जैसे- यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, लवण आदि को हटाकर मूत्र का निर्माण करना।
(ii) शरीर में जल संतुलन बनाए रखना।
24. समजात अंग और समवृत्त अंग में अंतर स्पष्ट करें।
Ans- समजात अंग और समवृत्त अंग में अंतर—
समजात अंग
(i) विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर एक समान होते हैं, भले ही उनके कार्य भिन्न-भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं।
(ii) उदाहरण – पक्षी के डैने तथा मनुष्य के अग्र पाद।
समवृत्त अंग
(i) विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जो रचना उत्पत्तियाँ उद्भव के दृष्टिकोण से एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। ऐसे अंग समवृत्त अंग कहलाते हैं।
(ii) उदाहरण – तितली के पंख तथा पक्षी के पंख।
25. जैव आवर्धन क्या है ? क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न-भिन्न होता है।
Ans- विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश कर विभिन्न पोषी स्तरों में उत्तरोत्तर सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं।
हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि रसायनों का छिड़काव करते हैं, इनका कुछ भाग मिट्टी द्वारा भूमि में रिस जाता है जिसे पौधे जड़ों द्वारा खनिजों के साथ ग्रहण कर लेते हैं, इन्हीं पौधों के उपयोग से वे रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा पौधों के लगातार सेवन से उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है जिसके परिणामस्वरूप जैव-आवर्धन का विस्तार होता है।
26. अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उसके कार्य लिखें।
Ans- अग्न्याशय द्वारा स्स्रावित हार्मोन
(i) इन्सूलिन का कार्य — रक्त में उपस्थित शर्करा की आधिक्य मात्रा को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर यकृत में संचित करना अर्थात रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करना।
(ii) ग्लूकागॉन का कार्य — ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर रक्त में शर्करा की मात्रा को बढाना।
27. परागण किसे कहते हैं ? स्वपरागण और पर परागण में अंतर स्पष्ट करें
Ans- परागण – पुष्प के नर जनन अंग पुंकेसर स्थित परागकोष से परागकणों का निकलकर मादा जनन अंग स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं।
- परागण निम्न दो प्रकार के होते हैं- (i) स्वपरागण (ii) परपरागण
स्वपरागण और पर परागण में अंतर
स्वपरागण
(i) परागकोष सेपरागकण निकलकर उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं।
(ii) परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है।
परपरागण
(i) परागकोष से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे, चाहे वे उसी जाति के हों या अन्य जाति के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं।
(ii) परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है।
28. ओजोन के अवक्षय के क्या कारण है ?ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव क्या है ?
Ans- ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण फ्लोरोकार्बन (FC) तया क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) नामक रसायन है जो ओजीन (O3) से अभिक्रिया कर उसका क्षय करता है। इससे सूर्य की घातक किरणें धरती पर सीधे पहुँचकर कैंसर जैसे रोग को बढ़ाएँगे।
ओजोन स्तर के अवक्षय से पराबैंगनी विकिरणें सीधे पृथ्वी तक पहुँचती है जिसके कारण मनुष्य को अनेक घातक एवं जानलेवा बीमारियों के चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है इसलिए यह चिंता का विषय है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 29 एवं 30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही एक का उत्तर दें।
29. तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है ? एक सामान्य तंत्रिका कोशिका की संरचना का चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
Ans- तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को तंत्रिका 
कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं।
(i) संवेदी तंत्रिकोशिका : शरीर के विभिन्न भागों से यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाती है।
(ii) प्रेरक तंत्रिकोशिका : यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक पहुँचाती है।
(iii) बहुध्रुवी तंत्रिकोशिका : यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से
पेशियों की ओर ले जाने का कार्य करती है।
30. मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित रेखाचित्र खींचे तथा उसके कार्यों का वर्णन करें।
Ans- नर-जनन तंत्र के विभिन्न भागों का कार्य निम्नवत है-

(1) वृषण : वृषण की कोशिकाएँ शुक्राणुओं को उत्पन्न करती हैं।
(ii) अधिवृषण : इसमें शुक्राणु संचित रहते हैं। अधिवृषण अन्तिम रूप से एक नलिका में रूपान्तरित होता है जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं।
(iii) शुक्रवाहिका : यह मांसल और संकुचनशील दीवारों वाली एक पतली नली होती है जो मूत्राशय के चारों ओर घूमकर अन्तिम रूप से मूत्रमार्ग में खुलती है।
(iv) शुक्राशय : यह छोटी-छोटी, नलिकाओं से बनी हुई रचना है जो अधिक कुंडलित होती है। यह एक गाढ़े शुक्राशय द्रव का स्राव करती है जो शुक्राणुओं से मिलने के बाद वीर्य कहलाता है।
(v) पुरःस्थ : यह दोहरी पालियों वाली ग्रन्थि होती है जिसकी नलिकाएँ मूत्रमार्ग में खुलती हैं। यह पुरःस्थ द्रव का स्राव करती है जो एक क्षारीय पदार्थ होता है जो वीर्य से मिलकर पुरुष के मूत्रमार्ग एवं स्त्री की योनि की अम्लीयता को उदासीन कर देता है। इसमें विशेष प्रकार की गन्ध भी होती है।
(vi) काउपर ग्रन्थि : यह ग्रन्थि जोड़े में होती है और पुरःस्थ के ठीक नीचे स्थित होती है। इसका सम्बन्ध एक छोटे रास्ते से होकर मूत्रमार्ग से होता है। यह एक सफेद क्षारीय द्रव का स्राव करती है जो चिकना होने के कारण स्नेहक का कार्य करता है।
(vii) शिश्न : यह पुरुष की बाह्य जनन इन्द्रिय है जिसके भीतर मूत्रवाहिनी होती है। शिश्न की मूत्रवाहिनी मूत्र एवं वीर्य को बाहर निकालने का कार्य करती है। शिश्न के भीतरी मूत्रवाहिनी के दोनों ओर स्पांजी ऊतकों की तीन कतारें होती हैं जो रक्त से भर जाने के बाद शिश्न को कठोर बना देती हैं।
| My Official Website | Visit Now |
|---|---|
| Youtube Channel | Click Here |
| Whatsapp Channel | Click Here |
| Telegram Channel | Click Here |
| Instagram Id | Click Here |