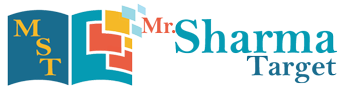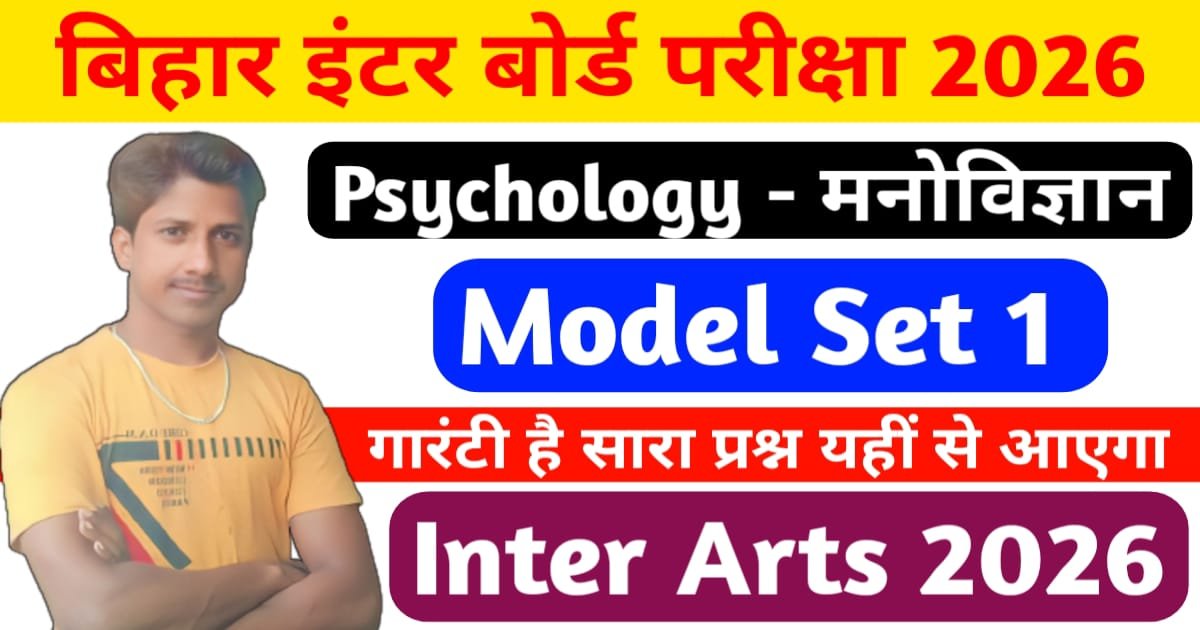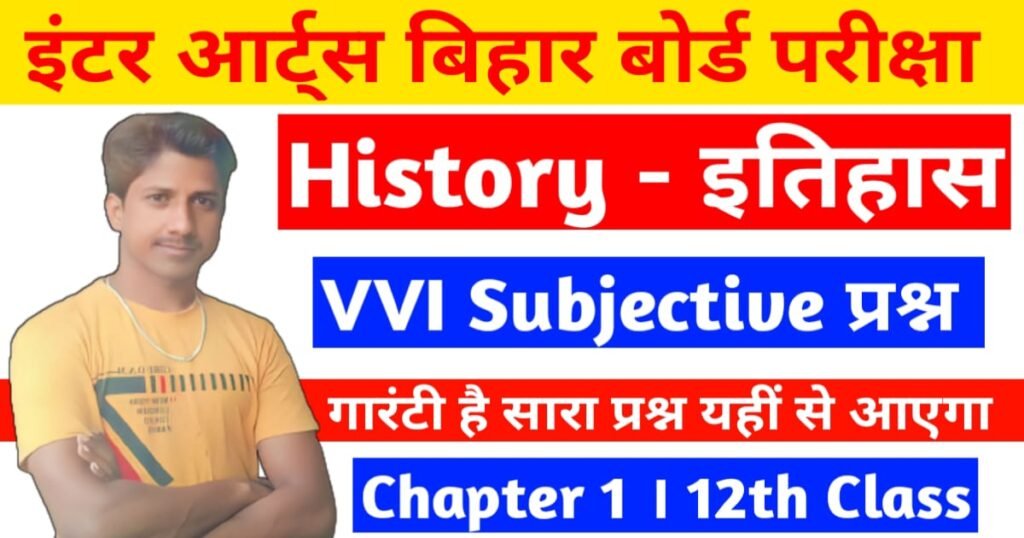Bihar Board 12th Class Psychology Subjective Question-Answer
यदि आप बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप शामिल होने वाले हैं तो यह पोस्ट आपके लिए ही है इस पोस्ट में हम आपको मनोविज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आसान भाषा में प्रश्न और उत्तर करने वाले हैं यदि आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में मनोविज्ञान में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस पोस्ट में जितने भी क्वेश्चन लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन किया जा रहा है सभी प्रश्न को अच्छे से कमांड कर लीजिए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्न इसी मॉडल सेट से आने वाले हैं।
| Subject | Psychology |
|---|---|
| Class | 12th |
| Model Set | 1 |
| Session | 2024-26 |
| Subjective Question | All Most VVI Questions |
-:- लघु उत्तरीय प्रश्न -:-
ध्यान दें :- प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से आपको किसी भी 10 प्रश्नों का उत्तर देना है।
1. अंतर समूह संघर्ष से आप क्या समझते हैं ?
Ans – अन्तर्समूह संघर्ष को सामाजिक संघर्ष भी कहते हैं। अन्तर्समूह का तात्पर्य उस सामाजिक परिस्थिति या समूह परिस्थिति से है, जहाँ परस्पर विरोधी घटनायें, प्रेरणायें, अभिप्राय, व्यवहार आवेग आदि होते हैं। अन्तर्समूह संघर्ष सदा सामाजिक परिस्थिति में होता है। अन्तर्समूह का आधार कोई लक्ष्य होता है। वह लक्ष्य प्रायः परस्पर विरोधी होता है। इस संघर्ष में सामाजिक शक्ति शामिल होती है। इस संघर्ष में तनाव होता है। अन्तर्समूह संघर्ष जानबूझकर किया जाता है।
2. सहभागी परीक्षण कौशल क्या है ?
Ans – प्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थ का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किया जाता है। प्रेक्षण के दो प्रमुख उपागम हैं-
- (i) प्रकृतिवादी प्रेक्षण और
- (ii) सहभागी प्रेक्षण।
3. मध्यप्णता संबंध विकार पर टिप्पणी लिखें।
Ans – मद्यपानता से शरीर दुर्बल हो जाता है। शरीर पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। विचार, चिन्तन, स्मरण तथा निर्णय शक्ति शिथिल हो जाती है। व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। अनिद्रा, चिन्ता, ऐंठन, ज्ञानेन्द्रियों की अतिशय क्रियाशीलता, कम्पन, विभ्रम, बेचैनी, पसीना आना, सिरदर्द आदि होने लगते हैं।
4. पराहम की विशेषताओं को लिखें।
Ans – पराहं की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं
(a) पराहं का संबंध नैतिकता से होता है पराहं किसी भी मूल्य पर अनैतिक एवं असामाजिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए राजी नहीं हो सकता है।
(b) पराहं चेतन, अर्द्धचेतन एवं अचेतन तीनों स्तर पर कार्य करता है : पराहं की एक विशेषता यह है कि यह चेतन, अर्द्धचेतन एवं अचेतन तीनों स्तरों पर कार्य करता है।
5. व्यवहार पर टेलीविजन के समाधान को लिखें।
Ans – मानव व्यवहारों पर दूरदर्शन के निम्नलिखित प्रभाव हैं-
टेलीविजन बड़ी मात्रा में सूचनाएँ और मनोरंजन को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करता है तथा यह दृश्य माध्यम है, अतः यह अनुदेश देने का एक प्रभावी माध्यम बन गया। इसके साथ ही चूंकि कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसलिए बच्चें उन्हें देखने में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। टेलीविजन देखने से बच्चों की एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता, उनकी सर्जनात्मकता तथा समझने की क्षमता तथा उनकी सामाजिक अंतः क्रियाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं। एक ओर, कुछ श्रेष्ठ कार्यक्रम सकारात्मक अंतः वैयक्तिक अभिवृत्तियों पर बल देते हैं तथा उपयोगी तथ्यात्मक सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं जो बच्चों को कुछ वस्तुओं को अभिकल्पित तथा निर्मित करने में सहायता करते हैं।
6. परामर्शदाता की विशेषताओं का वर्णन करें।
Ans – एक प्रभावी परामर्शदाता की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :
1. प्रमाणिकता : प्रमाणिकता का अर्थ है कि आपके व्यवहार की अभिव्यक्ति आपके मूल्यों, भावनाओं एवं आंतरिक आत्मबिम्ब अथवा आत्म छवि (Selfimage) के साथ संगत होती हैं। ये सभी बातें एक प्रभावी परामर्शदाता के पास होना चाहिए।
2. दूसरों के प्रति सकारात्मक आदर एक उपबंध्य परामर्शदाता संबंध में एक अच्छा संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। यह इस स्वीकृति को परावर्तित करता है कि दोनों की भावनाएँ अहम् हैं। इन भावनाओं को कम किया जा सकता है यदि परामर्शदाता सेवार्थी जैसा महसूस करता हो, उसके बारे में एक आदर का भाव प्रदर्शित करता है।
7. संवेगिक बुद्धि को परिभाषित करें। इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करें।
Ans – सांवेगिक बुद्धि एक तरह की ‘सामाजिक बुद्धि है। इस प्रकार की बुद्धि में स्वयं अपने एवं दूसरों के भावों को देखने-समझने, विभेद करने, अपनी सोच (चिंतन) एवं क्रिया को दिशा प्रदान करने हेतु सूचनाओं को उपधाग में लाने की योग्यता निहित रहती है। सन् 1990 में सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को औपचारिक रूप से प्रकाश में लाने और परिभाषित करने का प्राथमिक श्रेय सोलोवे एवं मेयर को जाता है।
सांवेगिक बुद्धि के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं –
(क) मनोभावों का प्रत्यक्षण मूल्यांकन एवं उन्हें व्यक्त करने की योग्यता
(ख) संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को मनोभावों द्वारा सुसाध्य या दक्ष बनाना
(ग) सांवेगिक सूचनाओं को समझना, विश्लेषण करना और भावात्मक ज्ञान को उपयोग में लाना, एवं
(घ) मनोभावों का नियमन करना
8. दमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
Ans – किसी अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति को समाप्त करने या कम करने के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली मनोरचनाएँ कही जाती हैं। जिसमें मुख्य मनोरचना दमन है। दमन मनोरचना के द्वारा व्यक्ति अपनी अप्रिय एवं समाज विरोधी इच्छाएँ, कटु स्मृतियाँ तथा घटनाओं को मन के चेतन स्तर से हटाकर अचेतन स्तर पर भेजता है। दमन द्वारा व्यक्ति उन समस्त इच्छाओं, विचारों आदि को अपने सक्रिय प्रयास एवं इच्छा द्वारा दबाने का भरसक प्रयास करता है जिन्हें वह अप्रिय, अनैतिक एवं दुखद समझता है।
9. सर्जनात्मकता को समझाइए।
Ans – सर्जनात्मक कार्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा समस्या को समझने, सूचनाओं को भंडारित करने और आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनः प्राप्ति करने के लिए न्यूनतम स्तर की योग्यता और क्षमता की जरूरत पड़ती है। उदाहरणार्थ सर्जनशील लेखकों को भाषा के उपयोग में दक्षता की जरूरत होती है। एक चित्रकार के लिए यह जानना लाजिमी है कि चित्र बनाने की उसकी एक विशेष तकनीक का दर्शक पर कैसा प्रभाव पैदा होगा, एक वैज्ञानिक को तर्कना में दक्ष होना चाहिए। इसलिए सर्जनात्मकता के लिए एक विशेष मात्रा में बुद्धि का होना जरूरी है लेकिन उस विशेष मात्रा से अधिक का सर्जनात्मकता से सहसंबंध नहीं होता।
10. बुद्धि मापन के एक वाचिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें।
Ans – बुद्धि-परीक्षण को दो भागों में बाँट सकते हैं-
(क) वैयक्तिक (ख) सामूहिक।
वैयक्तिक वाचिक उप-विभाजन में बीने साइमन ने काफी प्रसिद्धि पायी। एक तथा सामूहिक रूप से भी इसका प्रयोग होता है। शाब्दिक परीक्षणों में भाषा का प्रयोग होता है। जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता उसे क्रियात्मक परीक्षण कहते हैं। बीने साइमन माप में शाब्दिक, वैयक्तिक सामूहिक परीक्षण में आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण हुआ इसमें भाषा का प्रयोग होता है।
11. मानव व्यवहार पर टेलीविजन देखने के प्रभावों एवं मनोवैज्ञानिक समघात का वर्णन कीजिए।
Ans – टेलीविजन प्रौद्योगिकीय प्रगति का एक उपयोगी उत्पाद है, किन्तु उसके मानव पर मनोवैज्ञानिक समाघात के संबंध में दोनो ‘सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पाए गए हैं।
1. टेलीविजन बड़ी मात्रा में सूचनाएँ और मनोरंजन को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करता है तथा यह दृश्य माध्यम है, अतः यह अनुदेश देने का एक प्रभावी माध्यम बन गया। इसके साथ ही चूंकि कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसलिए बच्चे उन्हें देखने में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। इसके कारण उनके पठन-लेखन की आदत तथा घर के बाहर की गतिविधियाँ, जैसे-खेलने में कमी आती है।
2 . टेलीविजन पर हिंसा को देखना वस्तुतः दर्शकों में अधिक आक्रामकता से संबद्ध है। वच्चों में अनुकरण करने की उनमें प्रवृत्ति होती है किन्तु उनमें ऐसे व्यवहारों के परिणामों को समझने की परिपक्वता नहीं होती।
12. मानव व्यवहार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें।
Ans – आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का उपयोग अत्यधिक तेजी से बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का प्रभाव मानवीय व्यवहार एवं स्वास्थ्य दोनों पर पड़ा है। आधुनिक समाज विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण का शिकार हो रहा है। टेलीविजन, फ्रीज, वाशिंग मशीन, मोवाइल, लैपटॉप का प्रयोग घर-घर में हो रहा है जिससे मानव के व्यवहार और स्वास्थ्य दोनों में अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है उससे मानव के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं। इससे लोगों में चिन्ता, मनस्ताप, आक्रमकता अनुकरण जैसी बिमारियाँ पैदा हो रही हैं।
13. सामाजिक तनाव का वर्णन करें।
Ans – तनाव या प्रतिवल मनोविज्ञान के अनुसार एक मानसिक रोग है। यह व्यक्ति गत भी होता है और सामाजिक भी। जब किसी सामाजिक घटना या दुर्घटना के कारण तनाव उत्पन्न होता है तो उसे हम सामाजिक तनाव कहते हैं। इसमें समाज के अधिकांश सदस्य प्रभावित हो जाते हैं। सामाजिक तनाव उसे कहते हैं जिसके द्वारा बहुलांश व्यक्तियों के व्यवहार एवं अभिवृत्तियाँ काल्पनिक हो जाती हैं और उनसे लोग प्रभावित होते हैं। कभी-कभी प्रिन्ट मीडिया तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के कारण समाज में तनाव उत्पन्न हो जाता है।
14. भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है ?
Ans – भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) को 1986 में पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद को नीतियों व कार्यक्रमों को विनियमित करने, विकलांगता वाले व्यक्तियों को पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया। भारतीय पुनर्वास परिषद का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना है।
15. प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं ?
Ans – प्राकृतिक पर्यावरण एक ऐसा वातावरण है जिसमें सभी सजीव प्रजातियों और निर्जीव चीजों पृथ्वी या उसके क्षेत्र पर स्वाभाविक रूप से होने वाली बातें शामिल होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण अक्सर निवास स्थान के लिए एक पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है।
16. व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का वर्णन संक्षेप में करें।
Ans – व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि एक ऐसी प्रविधि है जो प्रेक्षणात्मक अधिगम पर आधारित है। इस प्रविधि में दूसरे व्यक्ति जैसे माता-पिता या चिकित्सक के परामर्शी एक खास व्यवहार करते देखता है तथा साथ ही साथ उस व्यवहार से मिलने वाले परिणामों से भी अवगत होता है। इस तरह के प्रेक्षण के आधार पर रोगी स्वयं भी वैसा ही व्यवहार करना धीरे-धीरे सीख लेता है। मॉडलिंग की यह विधि सुप्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक अलबर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है।
17. अभिवृत्ति की परिभाषा एवं इसके संज्ञानात्मक घटकों पर प्रकाश डालें।
Ans – अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है। यह किसी विशेष संबंध में विचारों का एक पूंज है जिसमें एक मूल्यांकन परक विशेषता (सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तटस्थता का गुण) पाई जाती है। इससे संबद्ध एक सांवेगिक घटक होता है। और अभिवृत्ति विषय के प्रति एक विशेष प्रकार से क्रिया करने की प्रवृति भी पाई जाती है। विचार परक घटक को संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है, सांवेगिक घटक को भावात्मक पक्ष के रूप में जाना जाता है और क्रिया करने की प्रवृत्ति को व्यवहारपरक अथवा क्रियात्मक घटक कहा जाता है। संक्षेप में इन तीनों घटकों को अभिवृति का ए-बी-सी घटक कहा जाता है।
18. समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक कर्म का वर्णन करें।
An s –जब दो समूहों में संघर्ष होता है तो उसे समूह संघर्ष कहते हैं। समूह संघर्ष के कुछ मनोवैज्ञानिक कारण निम्नांकित हैं-
1. दोनों पक्षों में संप्रेषण का अभाव एवं दोषपूर्ण संप्रेषण द्वंद्व एक प्रमुख कारण है।
2. सापेक्ष वंचन अंतर समूह संघर्ष का एक दूसरा कारण है। यह तब उत्पन्न होता है जब एक समूह के सदस्य स्वयं की तुलना दूसरे समूह के सदस्यों से करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि वे जो चाहते हैं वह उनके पास नहीं है परन्तु वह दूसरे समूह के पास है।
19. प्रेक्षक कौशल क्या है ?
Ans – अन्तर्दर्शन पद्धति में अपनी ही मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है किन्तु प्रेक्षण में हम दूसरों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन दूसरों के व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार क्रोधजनित उसके अनुभवों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। हमारा अपना अनुभव अन्तर्दर्शन द्वारा किए गये अपने मस्तिष्क के ऊपर आधारित होता है। हम अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर यह जानते हैं कि क्रोध के समय आँखें लाल हो जाती हैं, भौंहें तन जाती हैं, क्रोधित व्यक्ति गुस्से में चीखने लगता है तथा हाथों को इधर-उधर फेंकता है।
20. निर्धनता की परिभाषा दीजिए।
Ans – निर्धनता एक ऐसी दशा है जिसमें जीवन में आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है तथा इसका संदर्भ समाज में धन अथवा संपत्ति का असमान वितरण होता है।
-:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -:-
- ध्यान दें – प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको किसी भी तीन प्रश्नों का उत्तर देना है।
21. परामर्श क्या है ? परामर्श प्रक्रिया के चरणों का वर्णन करें।
Ans – परामर्श वास्तव में एक प्राचीन शब्द है। इसके अनेक अर्थ बताए गए हैं। वेबस्टर शब्दकोष के अनुसार “परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क-वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय है।” परामर्श में सहायतापरक संबंध होता है जिसमें सम्मिलित होता है वह जो मदद चाह रहा है, जो मदद दे रहा है या देने का इच्छुक है, जो मदद देने में सक्षम हो या प्रशिक्षित हो और उस स्थिति में हो जहां मदद लेना और देना सहज हो। राबिन्सन ने परामर्श की अत्यन्त स्पष्ट परिभाषा देते हुए कहा कि परामर्श में वे सभी परिस्थितियाँ सम्मिलित कर ली जाती हैं, जिनसे परामर्श प्रार्थी अपने आपको पर्यावरण के अनुसार समायोजित करने में सहायता प्राप्त कर सकें। वस्तुतः परामर्श दो व्यक्तियों से सम्बन्ध रखता है। परामर्शदाता तथा परामर्शप्रार्थी।
परामर्श प्रक्रिया के निम्नलिखित चस्ण हैं-
(i) परामर्शन की आवश्यकता का क्लायंट को अनुभव और परामर्शदाता के साथ साक्षात्कार हेतु समय निर्धारणः सर्वप्रथम क्लायंट को परामर्शन की आवश्यकता का बोध होना चाहिए; उसे अपने व्यवहार में किसी समस्या का प्रत्यक्षण और बाहरी सहायता (विशेषज्ञ परामर्शदाता) की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए।
(ii) पूर्व-परामर्शन साक्षात्कार/प्रथम-साक्षात्कार : क्लायंट और परामर्शदाता के मध्य प्रथम प्रत्यक्ष संपर्क अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण होता है। दोनों व्यक्ति सम्मिलित रूप में समय, सत्रों की संख्या, फीस जैसे बिंदुओं को स्पष्ट कर संविदा तैयार करते हैं। प्रथम साक्षात्कार के समय आकर्षण/विकर्षण, आशा/निराशा, और एक दूसरे के बारे में विश्वासों का बीजारोपण होता है। क्लायंट अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को परामर्शदाता के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा परामर्शदाता क्लायंट के साथ परामर्शन प्रक्रिया से संबंधित कार्य योजना और लक्ष्यों का निर्धारण करता है।
(iii) परामर्शन सम्बन्ध का विकास परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता और परामर्शी के मध्य व्याप्त सम्बन्धों की संरचना-जिसे परामर्शदाता सतर्कतापूर्वक विकसित करता है, का विशेष महत्त्व होता है। परामर्शन सम्बन्ध ‘व्यक्ति से व्यक्ति’ के मध्य एक कार्यात्मक सम्बन्ध होता है जिसमें परामर्शदाता में संगति और शक्ति पायी जाती है और वह क्लायंट को शक्ति संपन्न बनाने की चेष्टा करता है; क्लायंट के भीतर संगति को विकसित करने का प्रयत्न करता है।
(iv) परामर्शन के विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान: परामर्शन का अभीष्ट उद्देश्य सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा ही होता है, किन्तु तात्कालिक उद्देश्यों में भिन्नता हो सकती है। एक व्यक्ति की समस्या ‘लक्ष्यों की अस्पष्टता’ हो सकती है अतः उसे लक्ष्य के चयन में सहायता चाहिए।
(v) लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य-योजना का विकास और क्रियान्वयन : पूर्ववर्ती सोपान का स्वाभाविक विकास एक कार्य योजना का विकास करना होता है। परामर्शदाता लक्ष्य और सैद्धान्तिक उपागम के संदर्भ में उपयुक्त कार्य योजना का विकास करता है। कार्य योजना परामर्शदाता की समझ और परामर्शन उपागम के अनुसार विभिन्न रूपों में हो सकती है।
(vi) अनुवर्तनः सभी उपयुक्त प्रयत्नों के पश्चात भी समायोजनात्मक समस्याओं की पूर्ण या आंशिक पुनरावृत्ति (relapse) का खतरा होता है। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए परामर्शन सम्बन्धों के तकनीकी समापन के कुछ अन्तराल के बाद पुनः सम्पर्क स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाता है।
22. अंतर समूह संघर्ष के कर्म का वर्णन करें।
Ans – अन्तर्समूह संघर्ष के निम्नलिखित कारण हैं-
1. असमान के प्रति नापसन्दगी मनुष्य की यह एक प्रवृत्ति है कि वह अपने से भिन्न या असमान को पसन्द नहीं करता है। इसका आधार व्यक्ति की घृणा मूलप्रवृत्ति अथवा मृत्यु मूलप्रवृत्ति है। इसी मूल-प्रकृति से प्रभावित होकर एक समूह के लोग अपने से भिन्न समूह या समूहों के लोगों के प्रति नापसन्दी या घृणा की अभिव्यक्ति अपने वचन एवं व्यवहार के द्वारा करते हैं जो समूह-संघर्ष का मूल आधार या कारण है।
2. दोषपूर्ण पालन-पोषण समूह संघर्ष का एक कारण बच्चों को दोषपूर्ण पालन-पोषण की पद्धति है। मीड ने अपने अध्ययन के आधार पर बतलाया कि बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में पालन-पोषण की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है।
3. दोषपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था समूह संघर्ष अथवा सामाजिक संघर्ष को उत्पन्न करने में दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का भी हाथ होता है। दोषपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था के कारण भिन्न-भिन्न समूहों, वर्गों या सम्प्रदायों के प्रति विद्यार्थियों की मनोवृत्ति नकारात्मक, प्रतिकूल तथा आक्रामक बन जाती है।
4. धार्मिक विश्वास परस्पर विरोधी धार्मिक विश्वास भी समूह-संघर्ष अथवा सामाजिक संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण है। इतिहास साक्षी है कि धार्मिक कट्टरपन के कारण देश तथा विदेश में बड़े-बड़े युद्ध हुए हैं और कितने मासूम लोगों का खून बहा है।
5. राष्ट्रीय सम्पत्ति का असमान वितरण सधन तथा निर्धन के बीच संघर्ष एक लम्बे समय से आज तक जारी है और संभवतः यह कल भी जारी रहेगा। यदि दोनों के बीच आर्थिक दूरी को कम किया गया तो, अधिक सम्पत्ति वाले लोग कम सम्पत्ति वाले अथवा निर्धन लोगों पर अत्याचार करते हैं, तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं और उन आधिपत्य एवं प्रतिष्ठा का सिक्का जमाये रखना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।
23. मनोचिकित्सा के चरणों की विवेचना करें
Ans – मानसिक रोगों की चिकित्सा हेतु कई प्रविधियाँ भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर उपयोग में लाई जाती हैं। इन सभी प्रविधियों का उद्देश्य रोगी की चिंतन प्रक्रिया, संवेग, प्रत्यक्षीकरण, व्यवहारगत त्रुटियों आदि में सुधार लाना अथवा समायोजन लाना होता है।
मनोचिकित्सा के कई प्रकार होते हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :
(क) जैव-औषधीय मनोचिकित्सा : यह मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि मानसिक बीमारियाँ अंशतः जैविक कारणों से उत्पन्न होती हैं। अतः जैविक दोषों को नियंत्रित कर मानसिक बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। जैव-औषधीय चिकित्सा के अंतर्गत तीन प्रकार की प्रविधियाँ विशेष रूप से प्रचलित हैं, जैसे-
(i) इंसुलिन कोमा चिकित्सा : इस प्रविधि का उपयोग ‘मनोविदलता’ के रोगियों की चिकित्सा हेतु किया जाता था। वर्तमान समय में इस प्रविधि का उपयोग अत्यंत सीमित हो गया है।
(ii) विद्युत विक्षेपी चिकित्सा : इस प्रविधि में मेट्राजोल नामक द्रव्य की सुई लगाकर रोगी के शरीर में ऐंठन उत्पन्न करने का लक्षण पैदा किया जाता है। इस प्रविधि का विकास इस आधार पर किया गया कि चिकित्सकों की राय में रोगी को जब स्वतः झटका या ऐंठन मिलता है तो उनके असामान्य लक्षण अचानक दूर हो जाते हैं।
(iii) औषधि चिकित्साएँ : इस प्रविधि में प्रशान्तक दवाओं का उपयोग किया जाता है। 1960 के दशक में विषाद की अवस्था को नियंत्रित करने हेतु अवसाद विरोधी दवाओं का उपयोग होने लगा। आधुनिक समय में अन्य प्रकार के मनोरोगों-उन्माद विरोधी, दुश्चिता विरोधी एवं मनोविकृति विरोधी औषधियों का भी उपयोग होने लगा है।
(ख) मनोगत्यात्मक चिकित्सा : मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधि मनोरोगियों की चिकित्सा की आधुनिक मनोचिकित्सा प्रणाली है। इस प्रविधि को सिगमंड फ्रायड ने विकसित किया था। यह प्रविधि इस मान्यता पर आधारित है कि मानसिक समस्याओं की उत्पत्ति के पीछे बाल्यावस्था के अनुभवों का मुख्य हाथ रहता है।
(ग) व्यवहार चिकित्सा : इस प्रविधि में असामान्य व्यवहारों के कुसमायोजित स्वरूप को परिमार्जित कर समायोजित व्यवहार में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रविधि का विकास पावलॅव ने किया था।
(घ) संज्ञानात्मक चिकित्सा : इस प्रविधि में रोगी के कुसमायोजित व्यवहार के पीछे उसकी अविवेकपूर्ण विश्वास प्रणाली, जो एक लंबे समय से चलती आ रही होती है, की तहकीकात की जाती है और उसकी जगह विवेकपूर्ण विश्वास स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।
(ङ) योग चिकित्सा : योग चिकित्सा भारत की एक प्राचीन क्रियात्मक विचारधारा है। इसका उपयोग शारीरिक और मानसिक रोगों के निवारण हेतु किया जाता है।
24. मनोवैज्ञानिक प्रकार तथा स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव का वर्णन करें।
Ans – कई प्रभावों की प्रकृति शरीर क्रियात्मक होती है, लेकिन व्यक्तियों के भीतर अन्य परिवर्तन भी होते हैं। दबावपूर्ण स्थिति के साथ चार प्रमुख दबाव के प्रभाव संबद्ध हैं यथा संवेगात्मक शरीर क्रियात्मक, संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक। संवेगात्मक प्रभाव : वे व्यक्ति जो दबाव ग्रस्त होते हैं अक्सर आकस्मिक मनः स्थिति परिवर्तन का अनुभव करते हैं तथा सनकी के तरह व्यवहार करते हैं, जिसके कारण वे परिवार और मित्रों से विमुख हो जाते हैं। कुछ स्थितियों में इसके कारण एक दुश्चक्र शुक्र होता है जिससे विश्वास में कमी होती है एवं जिसके कारण फिर और भी गंभीर संवेगात्मक समस्याएँ पैदा होती हैं। उदाहरणार्थ, दुश्चिंता और अवसाद की भावनाएँ शारीरिक तनाव में वृद्धि, मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि और आकस्मिक मनः स्थिति में परिवर्तन। शरीर क्रियात्मक प्रभाव जब शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक द्वाव मनुष्य के शरीर पर क्रियाशील होते हैं तो शरीर में कुछ हारमोन यथा एड्रिनलीन और कॉर्टिसोल का स्राव बढ़ जाता है। ये हार्मोन हृदयगति रक्तचाप स्तर, चपापचय एवं शारीरिक क्रिया में विशिष्ट परिवर्तन कर देते हैं। जब हम थोड़े समय के लिए दवावग्रस्त हों तो वे शारीरिक प्रतिक्रियाएँ कुशलतापूर्वक कार्य करने में सहायता करती हैं, किन्तु दीर्घकालिक रूप में यह शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकती है। एपिनेफरीन और नॉरएपिनेफरीन छोड़ना पाचक तंत्र की धीमी गति, फेफड़ों में वायुमार्ग का विस्तार, हृदयगति में वृद्धि और रक्तवाहिकाओं का सिकुड़न, इस प्रकार के शरीर क्रियात्मक प्रभावों के मिसाल हैं।
संज्ञानात्मक प्रभाव यदि दबाव के कारण दाब लगातार रूप से बना रहता है तो व्यक्ति मानसिक अतिभार से ग्रस्त हो जाता है। उच्च दबाव के कारण उत्पन्न यह पीड़ा, व्यक्ति में ठोस निर्णय लेने की क्षमता को तेजी से घटा सकती है। घर में, जीविका में, अथवा कार्य स्थान में लिए गए गलत निर्णयों के द्वारा तर्क-वितर्क, असफलता, वित्तीय घाटा, यहाँ तक कि नौकरी की क्षति भी इसके परिणामस्वरूप हो सकती है। एकाग्रता में कमी और न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता भी दवाव का संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकता है।
व्यवहारात्मक प्रभाव दबाव का प्रभाव हमारे व्यवहार पर कम पौष्टिक भोजन करने, उत्तेजित करने वाले पदार्थों यथा कैफ्रीन का अधिक सेवन करने एवं सिगरेट, मद्य तथा अन्य औषधियों यथा उपशामकों इत्यादि के अत्यधिक सेवन करने में परिलक्षित होता है। उपशामक औषधियाँ व्यसन बन सकती हैं तथा उनके अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं यथा एकाग्रता में कठिनाई, समन्वय में कमी एवं घूर्मि या चक्कर आ जाना। दबाव के कुछ ठेठ या प्रारूपी व्यवहारात्मक प्रभाव, निद्रा-प्रतिरूपों में व्याघात, अनुपस्थितता में वृद्धि और कार्य निष्पादन में ह्रास हैं ।
25. व्यक्तित्व के सेल गुना की व्याख्या कीजिए।
Ans – व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से वर्णन करने से पहले, हमें उसके शीलगुणों को समझना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों का गुण से तात्पर्य ‘व्यवहार करने के ढंग से है। वुडवर्थ ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है, व्यक्तित्व गुण हमारे व्यवहार का एक मुख्य प्रकार का ढंग है, जैसे प्रसन्नता या आत्मविश्वास आदि जो कुछ समय तक तो हमारे व्यवहार के गुण ही होते हैं किन्तु कुछ दिनों बाद हमारे जीवन के एक अंग बन जाते हैं। वुडवर्थ व्यक्तित्व को इन्हीं गुणों का योग बताता है लेकिन इसके साथ ही साथ वह आगे यह भी बताता है कि व्यक्तित्व का तात्पर्य इस योग से कुछ अधिक भी है अर्थात् केवल योग ही व्यक्तित्व नहीं है वरन् व्यक्तित्व में कुछ और भी गुण सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति को जो प्रसन्न और आत्मविश्वासी है या दुखी है इसका तात्पर्य केवल यही नहीं कि वह इस प्रसन्नता, आत्मविश्वास या दुःख का योग है, वरन् वास्तव में वह इससे भी कुछ अधिक है।
व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त शील गुणों का गत्यात्मक संगठन है वे गुण निम्नलिखित हैं।
1. शारीरिक गुण : व्यक्ति के शारीरिक गुणों में उसकी लम्बाई चौड़ाई वरन् शारीरिक गठन आवाज, चेहरे की अभिव्यक्तियों, रंग, पोशाक आदि बातों को सम्मिलित किया जाता है।
2. मानसिक गुण : मानसिक गुणों में ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इन तीनों को संक्षेप में वर्णित करते हैं-
(अ) बुद्धि : व्यक्ति में बुद्धि एक प्रधान गुण होता है। प्रायः सामान्य बुद्धियुक्त व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी सामान्य हुआ करता है। निम्न कोटि के व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी निम्न कोटि का ही होता है तथा उच्च कोटि के व्यक्ति उच्च कोटि की बुद्धि वाले होते हैं। यह समाज को बुद्धि से शीघ्र प्रभावित कर लेते हैं।
(ब) स्वभाव : स्वभाव के आधार पर चार प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं-आशावादी, निराशावादी, चिड़चिड़े तथा अस्थिर। वास्तव में, व्यक्तियों में यह भेद संवेदनशीलता के आधार पर होता है जो व्यक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है।
(स) चरित्र: चरित्र व्यक्तित्व का एक विशेष अंग है। जिन व्यक्तियों का चरित्र दूषित होता है वे आकर्षण के पात्र नहीं होते। आदर्श चरित्र के व्यक्ति समाज में पूजे जाते हैं। महात्मा गाँधी इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।
3. सामाजिक गुण : व्यक्ति का जन्म समाज में होता है, अतः समाज ही उसके पालनपोषण का केन्द्र है। इस तरह से सामाजिकता उसका महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। कुछ व्यक्ति समाज से दूर भागना चाहते हैं तथा कुछ समाज में मिलकर चलते हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में सामाजिकता भिन्न-भिन्न मात्रा में होती है।
4. सशक्तता या दृढ़ता जिन व्यक्तियों में उपर्युक्त तीनों गुण विद्यमान हैं, लेकिन इन तीनों गुणों में दृढ़ता एवं सशक्तता नहीं है तो व्यक्ति को समाज में सफलता मिलनी असम्भव हो जाती है। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों में दृढ़ता होती है, वह जिन कार्यों को करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं उसे करके छोड़ते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है, समाज में वह आकर्षण के पात्र होते हैं। अतः दृढ़ता व्यक्ति का ही आवश्यक गुण है। उपर्युक्त सभी गुणों वाला व्यक्ति एक आदर्श व्यक्तित्व का धारक होता है। वह सभी कार्यों में सफल हो जाता है तथा समाज में सभी उसका आदर और सम्मान करते हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि वे समस्त गुण एक ही व्यक्ति में आमतौर से नहीं मिल पाते।
26. मनोवृतियों का निर्माण कैसे होता है ? इसके निर्धारकों का वर्णन करें।
Ans – मनोवृत्ति आनुवंशिक नहीं है, बल्कि एक अर्जित गुण है। व्यक्ति इसे अपनी अनुभव के आधार पर प्राप्त करता है। जैसे-जैसे व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है वैसे-वैसे उसकी मनोवृत्ति में भी विकास हो जाता है। इस प्रकार मनोवृत्ति का विकास व्यक्ति तथा वातावरण की परस्पर क्रियाओं का ही प्रतिफल है। अतः कहना न होगा कि इन परस्पर-क्रियाओं में जैविक तथा सामाजिक तत्वों का ही प्रधान हाथ रहता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों, जैसे कार्लसन, निम्कॉम्ब, मार्गन और रैमर्स ने मनोवृत्ति के सांस्कृतिक निर्धारकों पर अधिक जोर दिया है। उनके मतानुसार वह मनोवृत्ति जो विशेषकर सांस्कृतिक तत्वों से निर्धारित होकर समाज की अवस्थाओं के प्रति निर्देशित होती है, सामाजिक मनोवृत्ति कही जाती है। सांस्कृतिक तत्वों के अतिरिक्त प्रेरकों को संतुष्ट करने के क्रम में प्राप्त अनुभवों के कारण भी मनोवृत्ति का विकास होता है। अतः यहाँ मनोवृत्ति के कुछ मुख्य निर्धारकों का उल्लेख कर देना आवश्यक है-
1. प्रेरणात्मक निर्धारण : यह सर्वविदित है कि जन्मजात और अर्जित दोनों ही प्रेरकों से प्रेरित होकर व्यक्ति किसी विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करता है। जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय उसके लिए अनुकूल तथा प्रतिकूल का कोई अर्थ नहीं होता है। परन्तु जैसे-जैसे बच्चों में परिपक्वता आती जाती है, वैसे-वैसे उनमें भिन्नता भी आती जाती है। इस प्रकार उनमें किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था जाति आदि के प्रति एक मनोवृत्ति का विकास होता जाता है।
2. प्रत्यक्षात्मक निर्धारण : प्रत्यक्षीकरण का हाथ भी मनोवृत्ति का निर्धारण करने में अधिक रहता है। प्रत्यक्षीकरण के अनुसार ही मनोवृत्ति का विकास होता है। जिस वस्तु या संस्था के प्रति मनोवृत्ति का निर्माण होता है, उसका प्रत्यक्षीकरण भी किसी प्रत्यक्षात्मक, अवस्था में होता है।
3. मनोवृत्ति का वाचिक निर्धारक : मनोवृत्ति जन्मजात नहीं है, बल्कि अर्जित है। भाषा की सहायता या माध्यम से हम किसी दूसरे व्यक्ति की क्रिया, विचार, अनुभूति आदि को समझने में समर्थ होते हैं। अतः मनोवृत्ति-विकास की क्रियाएँ भी अधिकांशतः भाषा के द्वारा निर्धारित या प्रभावित होती हैं।