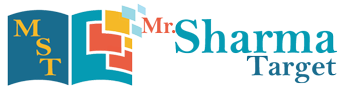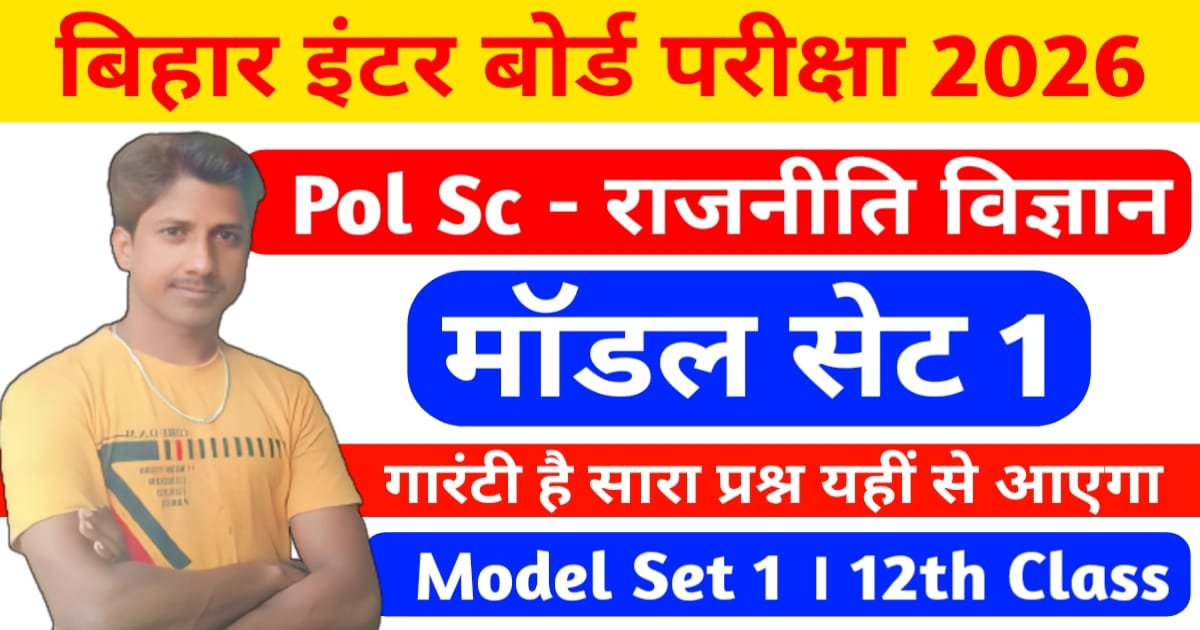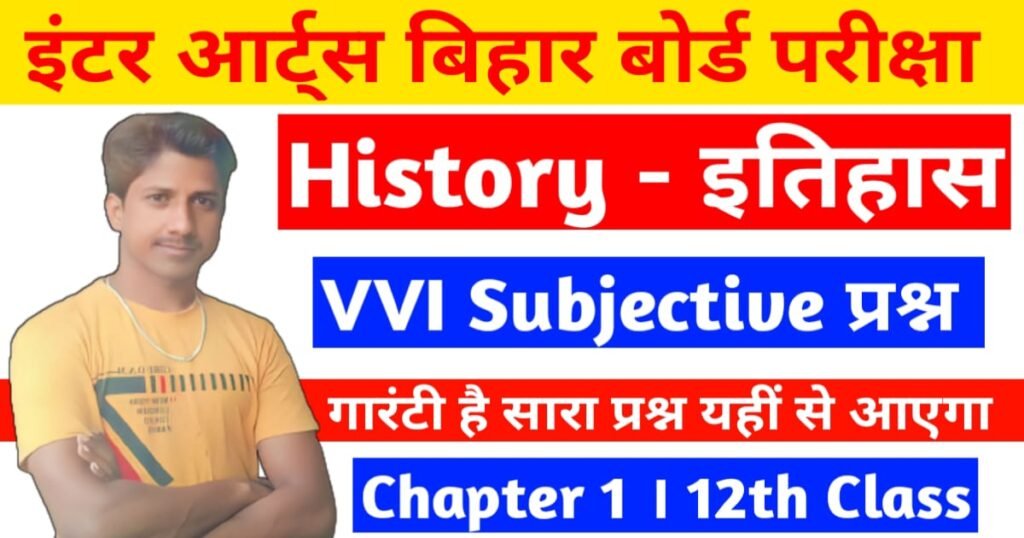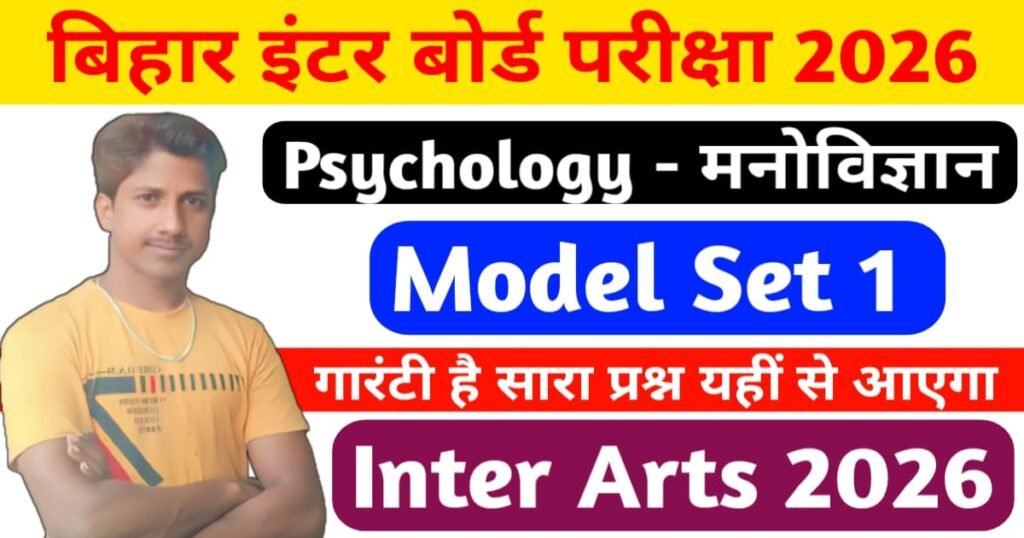Bihar Board 12th Class Political Science Model Set 1 Subjective – Answer
यदि आप बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप शामिल होने वाले हैं तो यह पोस्ट आपके लिए ही है इस पोस्ट में हम आपको राजनीतिशास्त्र का मॉडल सेट 1 लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आसान भाषा में प्रश्न और उत्तर करने वाले हैं। यदि आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में राजनीतिशास्त्र में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस पोस्ट में जितने भी क्वेश्चन लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन किया जा रहा है। सभी प्रश्न को अच्छे से कमांड कर लीजिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्न इसी मॉडल सेट से आने वाले हैं।
| Subject | Political Science - राजनीतिशास्त्र |
|---|---|
| Class | 12th |
| Model Set | 1 |
| Session | 2024-26 |
| Subjective Question | All Most VVI Questions |
Political Science – राजनीतिशास्त्र | Class 12 ( Arts ) | By-Suraj Sir
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही 15 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए दो अंक निर्धारित है।
1. चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखें।
Ans – चिपको आन्दोलन उत्तराखंड में जंगल के अधिकारियों के पक्षपाती व्यवहार के कारण से प्रारम्भ हुआ। जंगल के अधिकारियों ने ग्राम के लोगों को कृषि के यन्त्र बनाने के लिए लकड़ी काटने की अनुमति नहीं दी जबकि, उन्होंने खेल की सामग्री बनाने वाले ठेकेदारों को भूमिखंड ही दे दिया। इसके विरुद्ध ग्राम की महिलाओं ने अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। यह आन्दोलन मात्र कुछ लकड़ी की अनुमति ना मिलने से ही नहीं था। वास्तव में इसमें कई प्रकार के मुद्दे उठाये गये थे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय का व्यवहार था। ग्रामीणों को पूर्ति की जाने वाली शराब के विरुद्ध था व जंगल के अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ था। इसमें यह भी माँग थी कि स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय लोगों का ही अधिकार हो।
2. एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है।
Ans – 1991 से पूर्व विश्व में दो महाशक्तियाँ थीं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ के 15 राज्य अलग-अलग हो गये फलतः विश्वशक्ति के रूप में अमेरिका के मुकाबले सोवियत संघ का वर्चस्व समाप्तं हो गया। आज विश्व में हर क्षेत्र में अमेरिका की चौधराहट है। इसे ही एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं।
3. क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं ?
Ans – क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य अपने-अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों को भुला देना है। साथ-ही-साथ जो भी कमजोरियाँ या कठिनाइयाँ क्षेत्रीय देशों के सामने आएँ उन्हें परस्पर सहयोग से स्थानीय स्तर पर उनका समाधान ढूँढ़ने का प्रयास किया जाए।
4. तनाव शैथिल्य क्या है ?
Ans – कोरल बेल के अनुसार, “तनाव शैथिल्य का अभिप्राय है तनाव में सोच-समझकर और जान-बूझकर की गई कमी।” इसका आशय यह है कि तनाव में शिथिलता अचानक नहीं आई, यह निश्चित प्रयासों का परिणाम थी।
5. संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखें।
Ans – संयुक्त राष्ट्र संघ के दो उद्देश्य इस प्रकार है
1. अन्तर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध शांति और सुरक्षा को बनाए रखना।
2. आपसी तालमेल तथा सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना।
6. विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं ?
Ans – भारत एक अत्यन्त विशाल देश है। यहाँ लगभग 3000 जातियाँ निवास करती हैं, 179 भाषाएँ बोली जाती हैं और स्थानीय भाषाओं की संख्या लगभग
544 है। यहाँ अनेक धमों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। विभिन्न धर्मानुयायियों और सम्प्रदाय वालों के आचार-विचार, रहन-सहन, भाषा आदि में अन्तर होने के बाबजूद सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। अतः यह ठीक है कि यहाँ विविधता और भिन्नता के दर्शन होते हैं, परन्तु इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया जायेगा कि यहाँ विविधता में ही एकता है।
7. आर्थिक न्याय क्या है ?
Ans – आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक रूप है। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की आधारशिला है और समाज में रहने वाले लोगों में आर्थिक दृष्टिकोण से समानता ही आर्थिक न्याय कहलाता है। इस न्याय के अनुसार सम्पत्ति का समान और न्यायोचित वितरण समाज और राज्य के सभी व्यक्तियों के बीच होता है। यह न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है और सबको समान कार्य हेतु समान वेतन देने की व्यवस्था करता है। आज का प्रजातांत्रिक युग इसी न्याय पर आधारित है।
8. प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं ?
Ans – लोकतंत्र के दो रूप हैं- प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। देश के सभी नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होकर सरकार के मामलों पर विचार करते हैं और वाद-विवाद तथा निर्णय निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इस व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों के चुने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण, कर निर्धारण, अधिकारियों की नियुक्ति आदि का निर्णय करते हैं। स्वीटजरलैण्ड में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए देश को विभिन्न कैन्टनों में बाँटा गया है।
9. भूमंडलीकरण क्या है ?
Ans – व्यापार, वित्तीय प्रवाहों, टेक्नालॉजी और सूचनाओं के आदान-प्रदान से विश्व की अर्थव्यवस्था में समन्वय और एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है-प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं-विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुँचना, पूँजी का एक से ज्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई-कई देशों में पहुँचना और व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे जरूरी बात है-‘विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव’ जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है।
10. क्षेत्रवाद क्या है ?
Ans – क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की उस प्रवृत्ति से संबंधित है जो उनमें अपने क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक शक्तियों की वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टि से क्षेत्र देश का वह भू-भाग होता है जिसमें रहने वाले लोगों के समान उद्देश्य व आकांक्षाएँ होती हैं।
11. राष्ट्रपति की विधाई शक्तियां क्या है ?
Ans – राष्ट्रपति संसद का प्रमुख और आवश्यक अंग है। किसी भी कानून के निर्माण में उसकां सहयोग आवश्यक है। लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति ब्रिटेन के ताज के सदृश्य ही है। राज्य सभा के बारह सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है। दो आंग्ल प्रतिनिधियों को भी मनोनित करता है। लोक सभा में असम की आदिम जातियों तथा कुछ संघ प्रशासित क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधियों को वह मनोनीत करता है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन उसी के आदेश पर होता है। वह सदन में भाषण दे सकता है। किसी भी सदन में संदेश भेज सकता है। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर वह संयुक्त बैठक बुला सकता है। विधेयक पर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। अगर उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो संसद द्वारा पुनः पास हो जाने पर उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। वह वित्त या धन विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति देता है। संसद की अनुपस्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है।
12. विश्व व्यापार संगठन क्या है ? इसका उद्देश्य क्या है ?
Ans – विश्व व्यापार संगठन एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न देशों के बीच व्यापार को प्रोन्नत करने के लिए गठित किया गया है। इस संगठन की स्थापना 1995 में व्यापार तथा सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता (गैट) के उत्तराधि कारी के रूप में हुआ। इसका उद्देश्य बिना किसी भेद्भाव के समान रूप से खुले तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके सदस्य देशों की संख्या 150 है। इसका हर दो वर्ष बाद सम्मेलन होता है जिसमें व्यापार संबंधी चर्चाएँ की जाती हैं। इस संगठन को प्रजातांत्रिक तरीके से चलाया जाता है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। इसका अपना न्यायाधीकरण है जिसमें देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा होता है।
13. बहुदलीय व्यवस्था क्या है ?
Ans – भारत में ब्रिटेन अथवा अमेरिका की भाँति द्विदलीय प्रणाली नहीं है, | वरन् फ्रांस की तरह बहुदलीय प्रणाली है। लोकसभा में एक दर्जन से भी अधिक राजनीतिक दल हैं, विधानसभाओं में यह संख्या और भी अधिक है। भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस (आई), भारतीय साम्यवादी दल, मार्क्सवादी, दल को छोड़कर शेषदल अखिल भारतीय स्तर पर संगठित न होकर प्रांतीय स्तर पर ही संगठित हैं।
बहुदलीय पद्धति संसदात्मक सरकार के लिए हानिकारक है। संसदात्मक शासन में ब्रिटेन की भाँति एक शक्तिशाली विरोधी दल की बहुत आवश्यकता होती है। परन्तु भारत में इसका पूर्णतया अभाव है क्योंकि देश में अनेक राजनीतिक दल हैं और उनके थोड़े-थोड़े सदस्य ही संसद तथा विधान-मण्डल में हैं। इसका यह परिणाम है कि 1977 ई से पूर्व काँग्रेस दल की एक प्रकार से तानाशाही सी स्थापित हो गई थी और वह विधि-निर्माण तथा शासन सम्बन्धी नीति निर्धारण में अन्य दलों की पूर्ण उपेक्षा करती थी। आज भाजपा की सरकार में भी कमोवेश यही स्थिति है।
14. धन विधेयक क्या है ?
Ans – संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार वे विधेयक धन विधेयक माने. जाते हैं, जिसका निम्नलिखित विषयों से या इनमें से किसी एक से सम्बन्ध हो- (1) किसी टैक्स को लगाना, किसी टैक्स में वृद्धि करना या कोई परिवर्तन करना। (2) सरकार द्वारा ऋण लेने की व्यवस्था करना या आर्थिक देनदारी -लेना। (3) भारत के आकस्मिक निधि, संचित निधि के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करना। (4) भारत के संचित निधि में से किसी धनराशि को व्यय करना, (5) किसी सरकारी खर्च की भारत के संचित निधि पर डालंना या इस निधि से खर्च किये जाने वाले धन की मात्रा में वृद्धि करना आदि।
15. धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है ?
Ans – नये संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता, भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ ऐसे राज्य से होता है, जहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं होता और वह धार्मिक विकास के प्रश्नों में तटस्थ रहता है। धर्म निरपेक्ष राज्य का यह अर्थ नहीं कि भारत धर्म विरोधी राज्य है। इस सम्बन्ध में श्री वेंकटरमण का कथन विशेष उल्लेखनीय है कि, “धर्म-निरपेक्ष राज्य न धार्मिक है और न अधार्मिक, न धर्म विरोधी, परन्तु वह धार्मिक संकीर्णताओं और सिद्धांतों से सर्वथा पृथक है और इस प्रकार धार्मिक मामलों में पूर्णतः तटस्थ है।
16. संविधान एवं संविधान वाद में अंतर स्पष्ट करें।
Ans – संविधान से संविधानवाद की अभिव्यक्ति होती है और संविधान पर – ही संविधानवाद बहुत कुछ आधारित होता है।
संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है वहाँ संविधान एक संगठन का प्रतीक है। संविधान में किसी राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श निहित रहते हैं जबकि संविधानवाद में उन सिद्धांतों का संकलन पाया जाता है जिनके आधार पर शासन शक्तियों और शासकों के अधिकारों के सम्बन्धों का समायोजन होता है।
संविधानवाद में प्रधानता समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों की होती है, जबकि संविधान उन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधनों की व्यवस्था है और इस रूप में संविधानवाद और संविधान का परस्पर संबंध साध्य और साधन का है।
17. अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बताएं।
Ans – अधिकार के कई सिद्धान्त हैं जिनमें प्राकृतिक अधिकार प्रमुख है। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं, जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त थे। परन्तु ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों को आदर्श अधिकारों के रूप में माना है। उसके अनुसार ये वे अधिकार हैं, जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनकी प्राप्ति समाज में ही सम्भव है।
18. राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है ?
Ans – राजतंत्र में सर्वोपरि एवं अन्तिम सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है। गणतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में निहित रहती है। राजतंत्र सबसे प्राचीन शासन पद्धति है जबकि गणतंत्र आधुनिक। दुनिया के कम देशों में राजतंत्र है जबकि आज विश्व के ज्यादातर देश गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाये हुए हैं। राजतंत्र पुस्तैनी शासन पद्धति है जबकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है।
19. साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है ?
Ans – साम्यवादी अर्थव्यवस्था में निजी सम्पत्ति का अस्तित्व नहीं होता वहीं पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी सम्पत्ति की कोई सीमा नहीं होती। साम्यवाद में बाजार में कोई प्रतियोगिता नहीं होता। वहीं पूँजींवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता होती है जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार का कोई अस्तित्व नहीं होता वहीं पूँजीवादी अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार पर आधारित होता है।
20. निर्वाचन व्यवस्था में चार सुधार बताएं।
Ans – चुनाव आयोग द्वारा चुनाव व्यवस्था में निम्न सुधार अपेक्षित हैं :-
(i) ‘किसी भी अपराधिक छवि के व्यक्ति को उस पर किए गए F.I.R. के उपरान्त चुनाव नहीं लड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जब तक कानून द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है उसे चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता।
(ii) किसी भी राजनीतिक दल को किसी व्यवसायी से चंदा उगाही नहीं होनी चाहिए।
(iii) किसी भी नागरिक के लिए मतदान करना अनिवार्य होना चाहिए।
(iv) चुनाव से संबंधित गलत् घोषणा पत्र को एक अपराध माना जाना चाहिए।
21. नागरिक स्वतंत्रता क्या है ?
Ans – नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतन्त्रताओं से है जिनको एक व्यक्ति समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। गैटिल के शब्दों में “नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को कहते हैं, जिनकी सृष्टि राज्य अपने-अपने नागरिकों के लिए करता है।” सम्पत्ति अर्जित करने और उसे सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता आदि स्वतंत्रताएँ नागरिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती है।
22. न्यायिक सक्रियता क्या है ?
Ans – न्यायिक सक्रियता (Judicial activism) नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने का एक तरीका है जो न्यायाधीशों को सामान्यं रूप से प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में न्यायिक मिसाल के लिए कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित करता है। कभी-कभी ये निर्णय विधायी और कार्यकारी मामलों में घुसपैठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यायिक सक्रियता, निर्णयों के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा या विस्तार करने की न्यायपालिका में प्रथा है।
न्यायिक सक्रियता की अवधारण लोकहित याचिका (पीआईएल) की अवधारणा से निकटता से संबंधित है। यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता है।
23. बलवंत राय मेहता समिति के दो सिफारिश का उल्लेख करें।
Ans – बलवन्तराय जी मेहता द्वारा 1957 में सामुदायिक परियोजना के लिए निम्न सिफारिशें दी गई-
1. ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के साथ किया जाना चाहिए।
2. सभी नियोजन और विकासात्मक गतिविधियों को इन निकायों को सौंपा जाना चाहिए।
3. पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होनी चाहिए जबकि जिला परिषद सलाहकार, समन्वय और पर्यवेक्षी निकाय होनी चाहिए।
24. बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है ?
Ans – बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञापत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर-कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल. सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञापत्र अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके विरूद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। यह आज्ञापत्र गिरफ्तार हुआ व्यक्ति स्वयं या उसका कोई सहयोगी न्यायालय से याचना करके प्राप्त कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत मनमानियों पर रोक लगाकर साधारण नागरिकों को सुरक्षा देता है। मूलतः यह अंग्रेजी कानून में उत्पन्न हुई एक सुविधा थी जो अब विश्व के कई देशों में फैल गई है। ब्रिटिश विधिवेत्ता अल्बर्ट वेन डाईसी ने लिखा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिनियमों में कोई सिद्धांत घोषित नहीं और कोई अधिकार परिभाषित नहीं, लेकिन वास्तव में ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जमानत देने वाले सौ संवैधानिक अनुच्छेदों की बराबरी रखते हैं।”
25. राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है ?
Ans – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर है
- राज्य के पास अपनी जनता की चुनी हुई सरकार होती है जबकि केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्र सरकार कर्ताधर्ता होती है।
- प्रशासन चलाने के मामले में राज्य में मुख्यमंत्री प्रमुख होता है जबकि केन्द्र शासित प्रदेश में गवर्नर सरकार चलाता है गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
- संवैधानिक तौर पर प्रमुख व्यक्ति राज्य में गवर्नर होता है जबकि केन्द्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति प्रमुख, होता है।
- राज्यों में सत्ता की ताकत केन्द्र और राज्य सरकार में बंटी होती है जबकि केन्द्र शासित प्रदेश में सारी ताकत केन्द्र सरकार के पास होती है।
- क्षेत्रफल और जनसंख्या में राज्यों की तुलना में केन्द्र शासित प्रदेशों का. आकार छोटा होता है।
26. संप्रभुता क्या है ?
Ans – प्रभुसत्ता को हिन्दी में राजसत्ता अथवा संप्रभुता कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको सावरेन्टी कहा जाता है।
जेलिनेक के अनुसार – राजसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेशों से नहीं बँधता है।
27. कानून के स्रोतों का उल्लेख करें।
Ans – कानूनों के निम्नलिखित प्रमुख स्त्रोत हैं –
1. रीति-रिवाज एवं धर्म प्राचीन काल से ही धर्म एवं रीति-रिवाजों का बहुत अधिक महत्व है। इंगलैंड में कॉमन लॉ रीति रिवाजों एवं धर्म के कारण ही बना। पंजाब में भी महाराज रणजीत सिंह के समय रीति-रिवाजों को काफी महत्व रहा। आजकल भी पंजाब में रीति-रिवाजों की एक कानूनी पुस्तक है।
2. न्यायालयों के निर्णय कई बार न्यायाधीशों के पास ऐसे मुकदमें आ जाते हैं जिनका कानूनी रूप स्पष्ट नहीं होता है। वहाँ पर दोनों पक्षों के वकील कानून का अर्थ अपने-अपने पक्ष के हित में निकालते हैं। अतः विवादपूर्ण मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अपने फैसले देने पड़ते. हैं।
3. विधान मंण्डल : आधुनिक युग में कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत विधानमण्डल है। इन्हीं के द्वारा लोकतन्त्रीय देशों में कानून बनाये जाते हैं।
28. न्याय क्या है ?
Ans – प्लेटो ने न्याय की परिभाषा देते हुए कहा कि अपने निश्चित कर्त्तव्यों का पालन करना तथा दूसरे के कर्त्तव्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है।
प्लेटो का न्याय और कुछ नहीं बल्कि अपने कर्त्तव्यों का व्यवहार में प्रयोग है। प्लेटो की न्याय की परिभाषा काफी व्यापक है। क्योंकि यह इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना-अपना काम जो समाज द्वारा उस पर सौंपा गया है, करना चाहिए और उसे किसी दूसरे व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
29. दबाव समूह से आप क्या समझते हैं ?
Ans – समाज के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के हित, जैसे मजदूर, कृषक, भू-स्वामी, मिल मालिक, शिक्षक, व्यवसाय आदि होते हैं। इस वृहत श्रेणी के हित में अनेक छोटे-छोटे हित सम्मिलित होते हैं। जब समाज का छोटा या बड़ा संगठित रूप धारण कर लेता है तो उसे हित समूह कहा जाता है। जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार से सहायता माँगने लगता है या अपने सदस्यों के हितों के अनुकूल कानून निर्माण और संशोधन के लिए विधायकों को प्रभावित करने लगता है तब उसे हम दबाव समूह कहते हैं। ये अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार पर अनुकूल कानून-निर्माण के दबाव डालते हैं।
30. भारतीय विदेश नीति के तीन अनिवार्य कारक बताएं।
Ans – भारतीय विदेश नीति निश्चित करने के लिए निम्नलिखित तीन अनिवार्य कारक माने जाते हैं- 1: राष्ट्रीय हित, 2. राज्य की राजनीतिक स्थिति 3. पड़ोसी देशों से संबंध
Political Science – राजनीतिशास्त्र | Class 12 ( Arts ) | By-Suraj Sir
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 31 से 38 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 5अंक निर्धारित है।
31. भारत में विपक्षी दलों के उदय पर टिप्पणी लिखें।
Ans – संसदीय लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाने हेतु एक संगठित विरोधी दल की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से भारत में ब्रिटेन की तरह कोई विरोधी दल नहीं जो अकेले अपनी सरकार बना सके। भारत में सर्व-प्रथम विरोधी दल का निर्माण Prof. K. T. Shah के नेतृत्व में हुआ था जिसमें 14 सदस्य थे। 1952 ई० के निर्वाचन के बाद लोकसभा में नई विरोधी दल हो गये जिसमें साम्यवादी दल प्रमुख था परन्तु विरोधी दल को वैधानिक मान्यता इससे भी नहीं मिल सकी। मान्यता. प्राप्ति हेतु यह शर्त निश्चित की गयी थी कि लोकसभा में उस दल में लोकसभा की कुछ सदस्य संख्या के कम-से-कम 1/10 सदस्य होनी चाहिए। इस शर्त के अनुसार 1969 ई० में जब काँग्रेस विभाजित हो गई तो संगठन काँग्रेस की विरोधी दल की मान्यता मिली क्योंकि लोकसभा में संगठन काँग्रेस के 69 सदस्य थे। डॉ० राम सुभग सिंह इस विरोधी दल के नेता थे। 1971 ई० के निर्वाचन के बाद लोकसभा में कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त दल नहीं रह सका क्योंकि किसी भी दल को कुछ सदस्यों के 1/10 स्थान प्राप्त नहीं हो सके।
यद्यपि भारत में कोई एक संगठन विरोधी दल नहीं है। फिर भी संसदीय परम्पराओं के अनुसार विभिन्न छोटे-छोटे दलों ने सरकार की आलोचना करके कार्य स्थगन द्वारा बजट पर वाद-विवाद द्वारा वैदेशिक नीति पर चर्चा करके अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, अपने महत्त्व का परिचय दिया है।
संसद में विरोधी दलों ने कई बार अपना विरोध प्रगट किया है। संसद के दोनों में निरोधक नजरबन्दी कानून की अवधि तीन वर्ष और बढ़ा देने पर इसका तीव्र विरोध किया और इसे काले कानून की संज्ञा दी। गोवा विधेयक का जिसके द्वारा गोवा के भविष्य का निर्णय करने हेतु मत संग्रह का प्रस्तावना पारित हुआ है, तीव्र विरोध हुआ। जनसंघ ने कहा कि इससे सरकार पृथकता आदि प्रोत्साहित कर रही है। सरकार द्वारा रुपये के अवमूल्यन करने का घोर विरोध किया गया। 1966 ई० में श्री उमांशकर त्रिवेदी ने श्री मती गाँधी की सरकार पर अविश्वास प्रकट किया और आर्थिक स्थिति की कड़ी आलोचना की। श्री प्रकाश और वीर शास्त्री ने काश्मीर के बारे में संविधान की धारा 370 समाप्त करने की माँग की जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। विरोधी दलों के सदस्यों ने परमाणु बम बनाने की कई बार जोरदार माँग की है। पं० नेहरू के शासन काल में आपात काल स्थिति से उत्पन्न नजरबन्दी की समस्या को हल करने हेतु संविधान में संशोधन का विधेयक लाया गया परन्तु सदस्यों के विरोध पर भी श्री नेहरू ने उसे वापिस ले लिया था।
1980 ई० के बाद केन्द्र में लोकदल और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल की भूमिका निभा रही है। राज्यसभा में काँग्रेस (ई) के बहुमत में होने के कारण कार्यक्रम संचालन में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। भारत में पहली बार विरोधी दल के नेता को मंत्रि स्तर की सुविधाएँ प्रदान की गई है राजनीतिक दल संवैधानिक विरोधी के अलावा हिंसात्मक साधनों को अपने के लिए अपने समर्थकों को प्रोत्साहित करते हैं ।
32. राज्यसभा की संरचना अधिकार एवं कार्यों की समीक्षा कीजिए।
Ans – संगठन : राज्य-सभा संसद का ऊपरी सदन है। इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं-निर्वाचित और मनोनीत । संविधान की 80वीं धारा के अनुसार इनके सदस्यों की संख्या अधिक-से-अधिक 250 होगी। इनमें से अधिक-से-अधिक 238 सदस्य राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। राष्ट्रपति उन्हीं 12 व्यक्तियों को मनोनीत करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त किए हों। राज्यों के सदस्य-प्रतिनिधित्व-प्रणाली के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत-विधि द्वारा चुने जाते हैं।
राज्य सभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा के सदृश्य यह भंग होने वाली संस्था नहीं है। इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और उनमें से एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष के अन्त में अपने पद से हट जाते हैं और उनके स्थानों की पूर्ति नये सदस्यों के द्वारा हो जाती है। इस तरह का क्रम सदैव चलता रहता है जिसके कारण यह सभा हमेशा कायम बनी रहती है।
भारत का राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। वह अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। संसद उसे अपदस्थ कर सकती है। इसका एक उप सभापति भी होता है। राज्य सभा अपने सदस्यों में से किसी को इसके लिए निर्वाचित करती है। वह सभापति अनुपस्थिति में सभापति का आसन ग्रहण करता है। अगर उप-सभापति का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सभा उस पदं के लिए किसी दूसरे सदस्य को चुनती है। अगर राज्य सभा की बैठक में संभापति और उप-सभापति दोनों अनुपस्थित हों तो सभापति का कार्य वह संभालेगा जिसे राज्य सभा नियुक्त करे।
राज्य सभा के अधिकार और कार्य :
1. साधारण विधेयकों से सम्बन्धित अधिकार साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। कोई विधेयक उसी समय विधि बन सकता है। जब वह दोनों सदनों से पारित हो जाय।
2. वित्तीय और आर्थिक क्षेत्रों में अधिकार धन विधेयकों के सम्बन्ध में राज्य सभा को बहुत ही न्यून अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक और वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रारम्भ नहीं किये जा सकते। राज्य सभा न तो इन विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है और न संशोधित ही।
3. कार्यपालिका से सम्बन्धित अधिकार देश की वास्तविक कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राज्य सभा का मंत्रि-परिषद पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं रहता है।
4. संविधान में संशोधन सम्बन्धी अधिकार संविधान के संशोधन में राज्य-सभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है। संशोधन का प्रस्तात्न राज्य सभा में पेश किया जाता है फिर इसको पारित करने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का प्राप्त होना संविधान के अनुसार आवश्यक है।
5. आपातकालीन उद्घोषणा से सम्बन्धित अधिकार आपातकाल की उद्घोषणा की स्वीकृति राज्य सभा से प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।
33. भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों पर प्रकाश डालिए।
Ans – संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में हुआ। इसके बाद फ्रांस के संविधान में कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था हुई और फिर कालान्तर में आयरलैंण्ड, जर्मनी, रूस आदि देशों के संविधानों में।
भारतीय नगरिकों के मूल अधिकार निम्न हैं : 1. समानता का अधिकार, 2. स्वतंत्रता का अधिकार, 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और 6. सांवैधानिक उपचारों का अधिकार।
1. समानता का अधिकार इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से
अनुच्छेद 18 में है। फिर इसको पाँच अलग-अलग विभागों में विभक्त किया गया है।
(क) कानून के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिकों को कानून की नजर में समता और कानून का समान संरक्षक प्रदान किया गया है। कानून के नजर में सभी नागरिकों पर एक ही प्रकार के कानून होंगे तथा धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष कोई सुविधा नहीं दी जायेगी औरः कानून सभी नागरिकों का सम्मान रूप से संरक्षित करेगा। इस तरह यहाँ इंगलैंड की तरह विधि के शासन की स्थापना हुई।
(ख) सामाजिक समता अनुच्छेद 15 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर होटल, दूकान, भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सरकारी सहायता प्राप्त कुँओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, पाकों तथा अन्य सार्वजनिक उपभोग के स्थानों पर जाने से वंचित नहीं किया जायेगा।
(ग) अस्पृश्यता का अन्त: अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का सदा के लिए अन्त कर दिया गया है।
(घ) सार्वजनिक पदों की प्राप्ति में अवसर की समानता : अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को राज्य के अन्तर्गत सभी नौकरियों एवं सार्वजनिक सेवा के पदों की प्राप्ति का समान अधिकार कर दिया गया है। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर. विभेद नहीं किया जायेगा।
(ङ) उपाधियों का अन्त: अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना तथा विद्या-सम्बन्धी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अन्त कर दिया गया है।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) : भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है, अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रताएँ प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित सात स्वतंत्रताएँ प्रदान की गयी हैं-
(क) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है।
(ख) शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शान्तिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्यों के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है।
(ग) समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता : संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है, परन्तु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबन्धों के आधीन है, जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करें अथवा शान्ति और व्यवस्था को भंग करें।
(घ) भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता: भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबन्ध या विशेष अधिकार-पत्र के सम्पूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है।
(ङ) भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता : भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबन्ध या विशेष अधिकार-पत्र के सम्पूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।
34. भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें।
Ans – जातिवाद ने प्रारम्भ से ही भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इसने कभी राजनीति के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ा है तो कभी स्वयं में समस्या बनकर राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक हो गया है। यदि जातिवादी प्रवृत्ति किसी भी राज्य की राजनीति से समाप्त हो जाती है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार को तथा संकीर्णता को बड़े पैमाने पर दूर किया जा सकता है। हाल के कुछ वर्षों में इस प्रवृत्ति ने भारतीय संस्कृति और एकता को झकझोर दिया है।
स्वाधीनता के बाद राजनीतिक़ क्षेत्र में जातियों का प्रभाव पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण है। चूँकि अधिकांश भारतीय जनता आज भी अर्द्धशिक्षित है औरं परम्पराओं तथा रूढ़ियों में विश्वास करती है, इसलिए राजनीति की नई शब्दावली को वह आधुनिक सन्दर्भ में नहीं समझ पाती। सिर्फ परम्परागत राजनीति की ही भाषा को वह समझती है, जो जाति के चारों तरफ घुमती है। भारतीय वर्ण या जाति की प्रतिछाया है।
भारतीय जाति-व्यवस्था विशेषकर बिहार के सम्बन्ध में आज दो प्रश्न उठाए जाते हैं-जातिप्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जातिगत समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। रजनी कोठारी ने लिखा है कि ‘जो लोग राजनीति में जातिवाद की आलोचना करते हैं, वे न तो राजनीति के प्रचलित स्वरूप को भलीभाँति समझ पाए हैं, न जाति के स्वरूप को।’ उनके अनुसारं राजनीति में जातिवाद का राजनीतिकरण है। दूसरी तरफ राजनीति द्वारा जाति को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिला है। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए जाति संगठनों का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो जाति और राजनीति को परस्पर विरोधी के रूप में देखते हैं।
भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर विचार करने के लिए जाति के राजनीतिक रूप पर विचार करना आवश्यक है। जाति प्रथा के लौकिक रूप के अन्तर्गत जांति के अन्दर विवाह, छूआछूत और रीति-रिवाज के द्वारा जाति की पृथक इकाई कायम रखने का प्रयास सम्बन्धित है। भारत में देश की राजनीति पर किसी एक जाति की प्रधानता कभी नहीं रही है।
जाति का दूसरा पहलू व्यक्ति को समाज से बाँधता है। जातिप्रथा न सिर्फ जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को समाज में स्थान दिलाती है, वरन् इससे सभी तबके के व्यक्ति का समाज में लगाव पैदा हो जाता है। लोकतंत्रीय समाज के अन्दर विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए प्रतिद्वन्द्वितां होती है, इसमें विभिन्न समूहों या जातियों में एक-दूसरे से मिलने और गठबंधन करने की प्रेरणा भी देती है।
जाति-प्रथा का तीसरा तत्व चेतनाबोध है। हर जाति नवीण संस्कारों को अपनाकर ऊपर की जाति के समकक्ष स्थान ग्रहण करना चाहती है और इस प्रकार अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। किसी-किसी राज्य में उच्च जातियों के नकल न करने और राजनीति में सीधे प्रवेश की प्रवृत्ति मिलती है। उन इलाकों में जहाँ ब्रह्मणवर्ग पिछड़ा रहा, अन्य जातियाँ सीधे राजनीति में भाग लेने लगी और नेतृत्व की बागडोर उनके हाथों में आ गई। नए शासकवर्ग ने ऊँची जातियों के प्रभाव को स्वीकार किया और उनको राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवसाय में भाग लेने दिया। इस प्रकार पुराना समाज नई राजनीतिक व्यवस्था के करीब आया।
आज जातिगत राजनीति ने अपनी तमाम अवधारणाओं के बावजूद भारतीय राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। हरियाणा तथा बिहार की राजनीति में व्यक्तित्व और सैनिक सेवा के अतिरिक्त जातिगत प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। बड़ी संख्या में सेवा में भर्ती होने के चलते इस राज्य में जाति और वर्ग की भावना को काफी बल मिला है। इम तत्वों ने जातियों को संगठित क़िया। जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को, चुनावों के दौरान सुनने को मिला है। अन्य जातियाँ भी इस प्रवृत्ति का शिकार है। जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, जातिवाद ने वहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इस राज्य में जाति का राजनीतिकरण सबसे पहले हुआ। उत्तर प्रदेश में जाटो और ब्राह्मणों का प्रभाव राजनीति पर रहा है। निष्कर्षतः भारतीय राजनीति जातिगत भावनाओं से काफी प्रभावित है।
35. स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष क्या चुनौतियां थी।
Ans – ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय समाज को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया। अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया था कि भारत में ऊँच-नीच की भावना व्याप्त है व भारतीय समाज, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है। अतः उन्होंने इस बात का फायदा उठा कर भारत में शासन करने के लिए फूट डालो व राज करो की नीति अपनाई जिसमें वे सफल भी हो गये। अंग्रेजों ने भारत में आपसी द्वेष बनाए रखने के लिए जातिप्रथा को बढ़ावा दिया व साम्प्रदायिकता के बीज बो दिये। अंग्रेजी शासन की प्रत्येक नीति व कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि नीति को इस प्रकार से बनाया जाये व लागू किया जाये कि भारतीय समाज सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्तर पर बँटा रहे व उनमें असमानता व दूरी कायम रहे। अंग्रेजों के इन्हीं प्रयासों से मुस्लिम लीग जो एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था बाद में साम्प्रदायिक राजनीतिक दल बन गया जिसने अन्ततः पृथक् राज्य अर्थात् पाकिस्तान की माँग रख दी। इसी प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना जो एक धर्मनिरपेक्ष व राष्ट्रवादी व उदारवादी नेता थे, अंग्रेजों ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करके उनमें साम्प्रदायिक व स्वार्थी दृष्टिकोण पैदा कर दिया। वे केवल मुसलमानों के ही नेता बन कर रह गये जबकि प्रारम्भ में उनका दृष्टिकोण व्यापक था। अंग्रेजों की यह साम्प्रदायिक नीति ही भारत के विभाजन का प्रमुख कारण बना।
आजादी के बाद भारत के लिए राह आसान नहीं थी। उसके सामने अनेक चुनौतियाँ मुँह खोले खड़ी थीं। आजादी के समय महात्मा गाँधीजी ने कहा था कि, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जायेगें, लेकिन आधी रात को भारत का बँटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गाँधीजी ने भी आगे आने वाली समय की चुनौतियों की ओर संकेत दिया। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भारत के सामने भारत जैसे विशाल देश को राष्ट्र के रूप में बनाना व उसे निश्चित करना कि विभिन्न जाति धर्म, भाषा, संस्कृति व भौगोलिकता वाले लोगों में राष्ट्रीयता अर्थात् भारतीयता के सूत्र में बांध कर उन्हें एकता के सूत्र में बांधना था। अतीत के बहुत दुखद अनुभव रहे। एकता के अभाव में हमनें विदेशी लोगों का शासन पाया था अतः सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में एक रखना तथा सभी वर्गों के लोगों में आपसी प्यार बढ़ाना।
दूसरी चुनौती भारतीय प्रशासकों के लिए भारत में प्रजातंत्रीय प्रणाली के लिए आवश्यक राजनीतिक संस्कृति का विकास करके प्रजातंत्र को मजबूत करना था। जिसमें भारत काफी हद तक सफल रहा है। अब तक 75 वर्ष के प्रजातंत्रीय सफर में भारत में अनेक स्तर पर अनेक चुनाव होते रहे हैं जिससे भारतीय लोकतंत्रं परिपक्व हुआ। भारत का नागरिक मतदाता के रूप में भी परिपक्व हुआ है। भारत में प्रजातंत्र की जड़े मजबूत हुई हैं। ये भी वास्तव में एक बड़ी चुनौती थी।
तीसरी प्रमुख चुनौती भारतीयों के विकास व जनकल्यांण की थी जब देश आजाद हुआ भारत में गरीबी बेरोजगारी व क्षेत्रीय असंतुलन व अनपढ़ता जैसी अनेक समस्याएँ थीं। उन सभी को दूर करने के लिए आवश्यक प्रयास किये गये हैं व लोगों के जीवन स्तर को उठाया गया है। गाँव व शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया है। 15
36. राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य है ?
Ans – भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए योजनागत विकास का मॉडल चुना गया, देश के लिए समग्र रूप से योजनाएँ बनाने, प्राथमिकताओं का निर्धारण करने तथा संसाधनों का आवंटन करके योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य निष्पादन करने के लिए मार्च 1950 में एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग द्वारा तैयार किये गए योजना प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद् दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग आयोग में स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त भारत सरकार के वित्तमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री आदि भी सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद् में राज्यों के मुख्यमन्त्रियों सहित योजना आयोग के सदस्य तथा केन्द्र सरकार के मंत्रियों को आमंत्रित किया जाता हैं।
आयोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व प्रमुख हैं- (i) विकास प्रक्रिया की रूपरेखा को परिभाषित करना; (ii) विकास एवं सहायक नीतिगत वातावरण के लिए रणनीति को रेखांकित करना; (iii) संवृद्धि एवं इसकी क्षेत्रक संरचना के लिए वृहत् आर्थिक पैरामीटर्स तैयार करना; (iv) विभिन्न क्षेत्रक क्रियाओं के लिए केन्द्रों एवं राज्यों के बीच संसाधनों को आवण्टित करना; (v) विशिष्ट परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं योजनाओं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सीधे तौर पर लागू किया जाना है, पर विचार करना।
योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को अन्ततः राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में चूँकि सभी राज्यों / केन्द्र-शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री / उपराज्यपाल / प्रशासक तथा सभी केन्द्रीय मंत्री भाग लेते हैं। इसलिए यह माना जा सकता है कि इस बैठक में योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया जो प्रारूप अनुमोदित किया जाता है, उस पर आम सहमति है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद् सार्वजनिक नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
37. ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें।
Ans – ग्राम-पंचायत की महत्ता भारतीय संविधान में, उसकी धारा 40 में स्वीकार की. गयी है। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्येक ग्राम में करने की कोशिश की जाती है। अगर किसी ग्राम की आबादी ज्यादा है तो वहाँ दो पंचायतों की स्थापना भी की जाती है और यदि आबादी कम है, तो कई ग्रामों को मिलाकर भी एक ग्राम पंचायत स्थापित की जाती है।
ग्राम पंचायत के कार्य :
1. सामान्य कार्य :
(i) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना; (ii) वार्षिक बजट तैयार करना; (iii) प्राकृतिक संकट में सहाय्य कार्य करने की शक्ति; (iv) लोक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना; (v) स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना; (vi) गाँवों के अनिवार्य सांख्यिकी का अनुरक्षण।
2. कृषि पशुपालन, मत्स्यं
(i) कृषि और बागवानी का विकास और उन्नति; (ii) बंजर भूमि का विकास; (iii) चारागाह का विकास; (iv) मवेशी की नस्ल, कुक्कुट और अन्य पशुधन में सुधार; (v) गव्यशाला, कुक्कुटपालन और सुअरपालन को बढ़ाना; (vi) गाँवों में मत्स्यपालन का विकास;
3. वनोद्योग, जंगल, ईंधन और चारा :
(i) सड़कों के किनारे और अपने नियंत्रणाधीन अन्य सार्वजनिक भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण; (ii) ईंधन के लिए वृक्षारोपन और चारा विकास; (iii) फार्म वनोद्योग को बढ़ाना; (iv) सामाजिक वानिकी का विकास।
4. खादी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग :
(i) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ाना; (ii) ग्रामीण क्षेत्रों के लाभके लिए जागरूकता शिविर, विचारगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन करना।5. ग्रामीण गृह-निर्माण एवं पेयजल :
(i) अपने क्षेत्राधिकार और भीतर गृह-स्थलों का वितरण। (ii) गृहों, स्थलों एवं निजी और सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण। (iii) पेयजल के कुओं, हौजों, जलाशयों और चापाकलों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण; (iv) जल प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण; (v) ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं का अनुरक्षण; (vi) ग्रामीण सड़क, नाली और पुलिया का निर्माण और अनुरक्षण;
5 . गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत :
(i) गैर-परम्परागत ऊर्जा स्कीमों का उन्नयन एवं विकास; (ii) बायो-गैस संयंत्र सहित सामुदायिक गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों का अनुरक्षण;
6 . गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :
(i) पूर्ण नियोजन तथा उत्पादक आस्तिओं आदि के सृजन के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रम में भाग लेना;
7 . शिक्षा :
(i) लोगों में जागृति उत्पन्न करना और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता;
(ii) प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उनका प्रबंधन। (iii) वयस्क साक्षरता को बढ़ाना। (iv) ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय। (v) सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाना।
38. सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे ?
Ans – सरकार और अधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक सूचना पाने का अधिकार का कानून 12 अक्टूबर, 2005 से देश में लागू हो गया। इस कानून के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े विषय की सूचना पाने के आवेदनों पर अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर उत्तर देना होगा।
विश्व में भारत ऐसा 55वाँ देश बन गया है, जिसके आरटीआई अधिनियम को दुनिया में चौथा सबसे अच्छा दर्जा दिया गया है। जनता को सरकार से सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। इस कानून का उद्देश्य सरकार में विभिन्न स्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अकुशलता को नियंत्रित करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र और प्रदेश के प्रशासनों के अलावा पंचायतों, स्थानीय निकाय और सरकार से धन पाने वाले गैर सरकारी संगठन भी आयेंगे। अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र को केन्द्रीय सूचना आयोग गठित करना होगा। इस आयोग के एक मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिक से अधिक दस केन्द्रीय सूचना आयुक्त होंगे।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता करने वाली एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इस समिति के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केन्द्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा। इस सूचना आयोग के आम कामकाज की देखरेख, दिशा-निर्देश और प्रबंधन जैसे मामलों की शक्तियाँ मुख्य सूचनां आयुक्त के पास होंगी, जिसे अन्य सूचना आयुक्त मदद करेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जम्मू कश्मीर के अवकाश प्राप्तं वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी वजाहत हबीबुल्ला को देश का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया।
देश में सूचना के अधिकार का कानून लागू होने के साथ ही अब देशवासियों को किसी विभाग, केन्द्र अथवा परियोजना से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। यह आवश्यक नहीं है कि सारी सूचनायें, शुल्क अदा करने पर मिल ही जायेंगी क्योंकि इस कानून में देश की एकता, अखंडता. और सुरक्षा सहित कई विशेष परिस्थितियों में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराने की छूट है। इस कानून के अंतर्गत सरकारी रिकॉर्ड के निरीक्षण की सुविधा भी है, इसके लिए शुल्क लगता है।
यदि आपको यह मॉडल पेपर पसंद आया हो तो इसे लाइक , कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ” धन्यवाद “
Important Links
| My Official Website | Visit Now |
|---|---|
| Youtube Channel | Click Here |
| Whatsapp Channel | Click Here |
| Telegram Channel | Click Here |
| Instagram Id | Click Here |