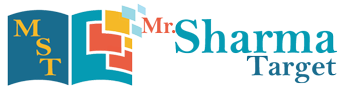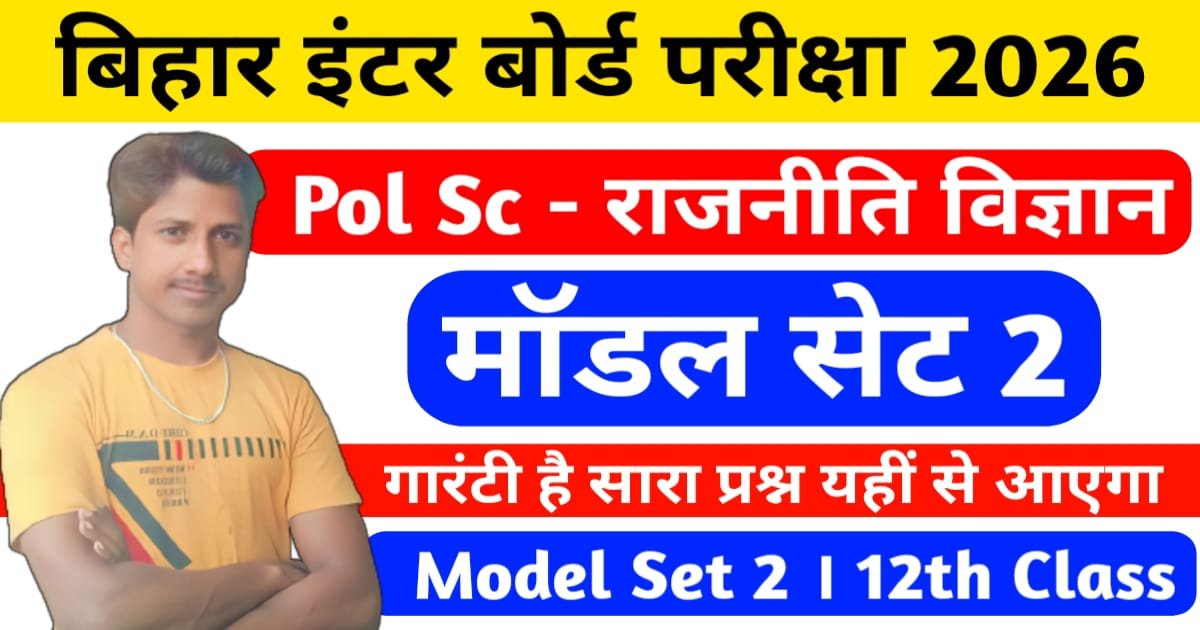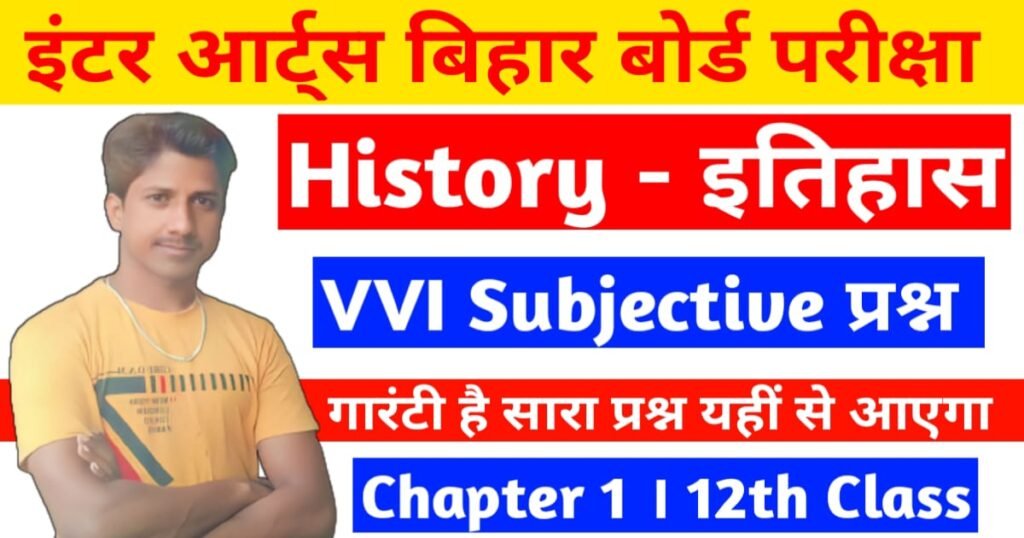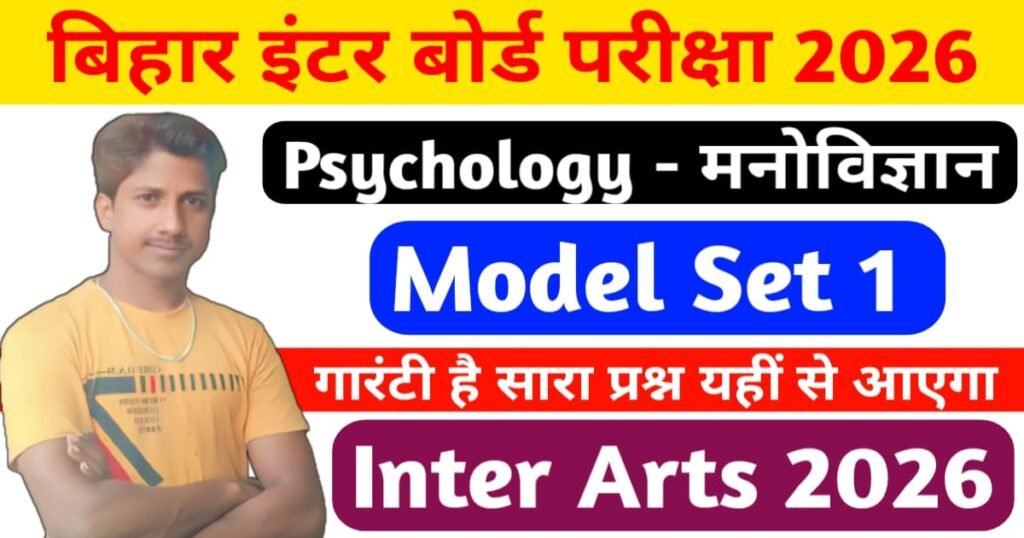Bihar Board 12th Class Political Science Model Set 2 Subjective -Answer
यदि आप बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप शामिल होने वाले हैं तो यह पोस्ट आपके लिए ही है इस पोस्ट में हम आपको राजनीतिशास्त्र का मॉडल सेट 2 लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आसान भाषा में प्रश्न और उत्तर करने वाले हैं यदि आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में राजनीतिशास्त्र में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस पोस्ट में जितने भी क्वेश्चन लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन किया जा रहा है सभी प्रश्न को अच्छे से कमांड कर लीजिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्न इसी मॉडल सेट से आने वाले हैं।
| Subject | Political Science - राजनीतिशास्त्र |
|---|---|
| Class | 12th |
| Model Set | 2 |
| Session | 2024-26 |
| Subjective Question | All Most VVI Questions |
Political Science – राजनीतिशास्त्र | Class 12 ( Arts ) | By-Suraj Sir
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही 15 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए दो अंक निर्धारित है।
1. दल बदल विरोधी कानून के मुख्य बिंदु क्या है ?
Ans- 1985 के दलबदल विरोधी कानून के बाद भी दलबदल की कुरीति पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा। अतः सन् 2003 में इसे रोकने के और कदम उठाए गए। सन् 2003 में संसद ने 91 वां संविधान संशोधन कानून पास किया जो प्रथम मई 2004 से लागू हुआ। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए-
1. किसी भी सांसद या विधायक को दल बदलने पर मंत्री के पद या किसी अन्य लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इससे मंत्री के पद की प्राप्ति के कारण दल-बदल पर रोक लगी।
2. यह भी व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा या संबंधित विधान सभा की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इसके द्वारा पूरे दल के द्वारा दलबदली या निष्ठा बदली पर रोक लगी।
2. खुली अर्थव्यवस्था क्या है ?
Ans- खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इसे विदेशी व्यापार भी कहते हैं। इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। इससे निवेशकों को घरेलू और विदेशी परिसम्पत्तियों के बीच चयन का अवसर प्राप्त होता है। इससे वित्तीय बाजार में सहलग्नता का निर्माण होता है। उदाहरण-भारत के लोग अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करते हैं। साथ ही भारतीय उत्पादन का कुछ भाग विदेशों को भी निर्यात किया जाता है।
3. एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है ?
Ans- एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ है कि लम्बे अन्तराल तक देश में किसी एक राजनीतिक दल का ही शासन रहना। 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से ही कांग्रेस का राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभुत्व रहा जो 1952 में सम्पन्न हुए प्रथम चुनाव से लेकर 2009 में हुए चुनावों तक देखा जा सकता है।
4. भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है।
Ans- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में संसद, राज्य विधान मंडल के. साथ-साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और निर्वाचन नामावलियों की तैयारी पर नियंत्रण रखने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अतः केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर निर्वाचन का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग पर है।
5. संक्षेप में परमाणु युद्ध के प्रभावों का वर्णन करें।
Ans- परमाणु युद्ध के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं-
(i) परमाणु अस्त्र न केवल युद्ध में लड़ने वाले देशों का बल्कि मानव मात्र का विनाश कर सकते हैं।
(ii) यदि सभी देशों की शक्ति इकट्ठी कर दें जिनके पास परमाणु बम हैं, तो वह शक्ति इतनी होगी कि सारे विश्व को कई बार नष्ट किया जा सकता है।
(iii) यदि विश्व में परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी मानव जाति नष्ट हो जायेगी।
6. निशस्त्रीकरण की परिभाषा दीजिए।
Ans-निःशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों/अस्त्र-शस्त्रों के उत्पागन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। शस्त्र नियंत्रण की दिशा में विभिन्न राष्ट्र प्रेरित होकर अपने शस्त्र भण्डारों में जो कमी कर रहे हैं तथा अपने सैनिक व्यय में जो कमी कर रहे हैं, ये सब प्रयास निः शस्त्रीकरण के अन्तर्गत ही आते हैं। जेनेवा में होने वाले निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
7. विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य बताएं।
Ans- विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1948 ई. में की गयी थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य विश्व के सभी देशों के नागरिकों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसका कार्यालय जेनेवा में है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
(i) नई-नई औषधियों की खोज करना।
(ii) नशीली वस्तुओं के प्रयोग की रोकथाम करना।
(iii) हैजा और तपेदिक जैसी बीमारी को खत्म करना।
(iv) संसार के सभी देशों को B.C.G. के टीके भेजने का कार्य करना।
8. गैर कांग्रेसी वाद से आप क्या समझते हैं ?
Ans- गैर-कांग्रेसवाद वह स्थिति थी जो विभिन्न विरोधी राजनीतिक दलों ने कांग्रेस के खिलाफ उत्पन्न की तथा इस बात के लिए वातावरण बनाने का प्रयास किया कि कांग्रेस के प्रभुत्व को कम किया जाये। विरोधी दलों ने विभिन्न राज्यों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हड़ताल, धरने व विरोध प्रदर्शन किये। गैर-कांग्रेसवाद के विकास का उद्देश्य यह भी था कि कांग्रेस के खिलाफ पड़ने वाले वोटों को विभाजित होने से रोका जाये क्योंकि गैर-कांग्रेसी वोट विभिन्न विरोधी दलों के उम्मीदवारों में ना बढ़ पाये जिससे कांग्रेस के उम्मीदवारों को इसका फायदा ना मिले।
9. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख करें।
Ans- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन विशेष परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ था। आरंभमें गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सार था परन्तु बाद में संसार को बड़े गुटों (अमेरिकी एवं सोवियत संघ गुट) में बँट जाने से इस गुटनिरपेक्षता ने एक आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। तब कुछ और देशों ने भी गुटनिरपेक्षता को सैनिक गुटों में बँटे संसार के लिए शांति दूत मान लिया। युद्ध के निकट आने वाले संसार को गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता थी। सैनिक हथियारों की होड़ न करने वाले देशों को गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता थी। भारत ने यह विदेश नीति व आंदोलन दोनों संसार को दिये थे।
10. सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं ?
Ans- काफी प्राचीनकाल से ही विद्वानों ने आर्थिक न्याय के साथ-साथ सामाजिक न्याय की धारणा पर विचार किया है। अरस्तू, कौटिल्य आदि के नाम इस संबंध में उल्लेखनीय हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के सामाजिक आंदोलनों ने इस धारणां को अधिक विकसित किया। फ्रांस की राज्य क्रांति ने सामाजिक न्याय का राजनीतिक स्वतंत्रता से घनिष्ठ संबंध जोड़कर इस’ अवधारणा को काफी महत्त्व प्रदान किया। वर्तमान काल में तो यह स्वीकार किया जा सकता है कि विश्व शांति की स्थापना सामाजिक न्याय के आधार पर ही संभव है। संयुक्त राष्ट्रसंघ इस दिशा में विशेष रूप से प्रयत्नशील है।
11. प्रस्तावना से क्या समझते हैं ?
Ans- विश्व के प्रत्येक देश के संविधान की अपनी एक प्रस्तावना होती है। इस प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के विचार एवं उद्देश्य के साथ-साथ संविधान तथा देश के मौलिक लक्ष्यों की अभिव्यक्ति रहती है। देश के आधारभूत दर्शन, मूल आस्थाएँ तथा नागरिकों की आकांक्षाओं का स्पष्टीकरण प्रस्तावनारूपी आईने में ही होता है। अतएव, प्रस्तावना संविधान के दर्पण के रूप में कार्य करती. है। संविधान की प्रस्तावना का वही महत्त्व है जो महत्त्व किसी पुस्तक की प्रस्तावना का होता है। इसीलिए, प्रस्तावना को ‘संविधान ‘की कुंजी’ कहा गया है, जिसका समर्थन अनेक विद्वानों ने किया है। प्रस्तावना संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है और उसके अस्पष्ट उपबन्धों के स्पष्टीकरण में सहायक होती है।
12. मौलिक अधिकारों का वर्णन करें।
Ans- अधिकार किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य की आधारशिला है। यह वह गुण है जिसके कारण राज्य की शक्ति के प्रयोग में नैतिकता का समावेश होता है और वह नागरिकों के आदर्श एवं सुखमय जीवन के लिए नितांत आवश्यक होता है।
भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार निम्न हैं
1. समता का अधिकार, 2. स्वतंत्रता का अधिकार, 3. शोषण के विरूद्ध अधिकार, 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, 6. सम्पत्ति का अधिकार और 7. सांवैधानिक उपचारों का अधिकार।
13. भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या है ?
Ans- भारत में केन्द्र तथा राज्यों की राजनीति में जात्तीयता का बोलबाला एक निर्धारक तत्व रहता है। जातीयता की भावना बड़े पैमाने पर आज दलबदल को प्रभावित कर रही है। जातीयता की इस संकीर्ण भावना ने राजनीति को अपवित्र कर दिया है। मुख्यमंत्रियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी जातीयता के संदर्भ में देखा जा रहा है। आज यह बात महसूस की जा रही है कि व्यक्ति चाहे किसी भी राजनीति दल या समूह में क्यों न हो, लेकिन जातीयता तथा सामूहिक भावना के कारण वे आज एक हो जाने को तत्पर हो जाते हैं। बिहार की राजनीति को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जब श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे और वे काफी विरोधों के बावजूद पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे रहे थे तब रामलखन सिंह यादव सहित सारे सामूहिक सदस्य उनको अपना नेता मानते थे। अतएव जातीय तथा सामूहिक भावना दलबदल को प्रोत्साहित करती है। इसी आधार पर आज भारत में अनेक राजनीतिक दल और नेता हो गये हैं।
14. भारत में दलीय व्यवस्था पर टिप्पणी लिखें।
Ans- मनुष्यों के उस संगठन को राजनीतिक दलं कहते हैं, जिसमें वे अपने सम्मिलित प्रयत्न द्वारा किसी ऐसे सिद्धांत पर राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करने हेतु संगठित होते हैं जिनके विषय में वे सहमत हैं। गेटेल के शब्दों में राजनीतिक दल नागरिकों का वह पूर्णतया या आशिक रूप से व्यवस्थित संगठन है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा शासन पर नियंत्रण करने के लक्ष्य से अपनी नीति को कार्यरूप देने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रत्येक राजनीतिक दल का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिसके आधार पर वह जनता में लोकंप्रिय होकर अपनी सरकार बनाना चाहता है।
15. ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें।
Ans- ग्राम पंचायत के कार्य निम्न हैं :
(i) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना;
(ii) कृषि और बागवानी का विकास और उन्नति;
(iii) मवेशी की नस्ल, कुक्कुट और अन्य पशुधन में सुधार;
(iv) चारागाह का विकास।
(v) वृक्षारोपण और चारा विकास
(vi) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ाना;
(vii) ग्रामीण गृह-निर्माण;
(viii) पेयजल के कुओं, हौजों, जलाशयों और चापाकलों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण;
(ix) जल प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण;
16. राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं ?
Ans- भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए योजनागत विकास का मॉडल चुना गया, देश के लिए समग्र रूप से योजनाएँ बनाने, प्राथमिकताओं का निर्धारण करने तथा संसाधनों का आवंटन करके योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य निष्पादन करने के लिए मार्च 1950 में एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग द्वारा तैयार किये गए योजना प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता था। योजना आयोग (अब नीति आयोग) और राष्ट्रीय विकास परिषद् दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग में स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त भारत सरकार के वित्तमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री आदि भी सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद् में राज्यों के मुख्यमन्त्रियों सहित योजना आयोग के सदस्य तथा केन्द्र सरकार के मंत्रियों को आमंत्रित किया जाता है।
17. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बताएं।
Ans- कार्यपालिका, वित्तीय, व्यवस्थापिका तथा न्यायिक अधिकारों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को आपातकालीन सम्बन्धी महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। वह निम्नांकित तीन परिस्थितियों में आपातकालीन घोषणा कर सकता है-
(i) युद्ध या बाह्न आ मण अथवा आंतरिक अशांति या उसका खतरा होने पर
(ii) राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर
(iii) आर्थिक या वित्तीय संकट आने पर
उपर्युक्त वर्णित कुछ महत्वपूर्ण अधिकार भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदान किए हैं जो इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की भाँति देश का वास्तविक शासक बनाने में मदद करता है।
18. संघ केंद्र शासित क्षेत्र क्या है ?
Ans- भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून पारित किया। आयोग द्वारा की गई सिफारिश में थोड़ा हेर-फेर कर भारतीय संसद ने 31 अगस्त 1956 ई. को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया। इसे उसी साल के । नवम्बर को लागू किया गया। इसे प्रभावित करने के उद्देश्य से संविधान में कुछ संशोधन किए गए। इस अधिनियम द्वारा समस्त भारतीय क्षेत्र को केवल दो प्रकार की इकाइयों में विभाजित किया। इन्हें राज्य और संघ या केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र .. की संज्ञा दी गई।
अतः संघ शासित क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है जिसमें भारत सरकार का शासन होता है। भारत में कुल सात संघीय क्षेत्र हैं :
1. अंडमान निकोबार द्वीप 2. दिल्ली 3. चंडीगढ़ 4 दमन-दियु 5. पांडीचेरी 6. दादरा नगर हवेली तथा 7. लक्षद्वीप ।
जम्मू-कश्मिर तक लदाख वर्तमान में केन्द्रशासित प्रदेश बन गये हैं।
कुछ संघीय क्षेत्रों में भी विधानसभा की व्यवस्था है और उनमें संसदीय प्रकार की कार्यपालिका की व्यवस्था है जैसे कि पांडिचेरी में। अब दिल्ली में भी विधानसभा की व्यवस्था कर दी गई है।
19. गुटनिरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या है ?
Ans- भारत की विदेश नीति का एक मूल सिद्धान्त गुटनिरपेक्षता है। इसका अर्थ है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के सम्बन्ध में अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति का पालन करता है। सांरा विश्व 1991 तक दो गुटों में विभाजित था-एक अमेरिकी गुट तथा दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी विदेश नीत्ति में गुट निरपेक्षता के सिद्धान्त को अत्यधिक महत्त्व दिया। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को जन्म देने तथा उसको बनाए रखने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1961 से लेकर 24 फरवरी, 2003 द्वारा इसके 13वें शिखर सम्मेलन (कुआलालम्पुर) तक भारत ने इसको बराबर सशक्त बनाए रखने का प्रयत्न किया है। भारत प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का समर्थन या विरोध उसमें निहित गुण और दोषों के आधार पर करता रहा है। भारत ने यह नीति अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए अपनायी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत को अमेरिकन तथा पूर्व सोवियत संघ के गुटों ने अपनी ओर आकर्षित करने तथा अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया परंतु भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ।
20. संयुक्त राष्ट्र की महासभा के संगठन की विवेचना कीजिए।
Ans- महासभा संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च अंग है और एक प्रकार से विश्व की संसद के समान है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें पाँच प्रतिनिधि भेजता है, लेकिन उनका मत एक ही होता है। प्रायः वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होता है। इसकी स्थापना के समय इसके सदस्यों की कुल संख्या 51 थी जो बाद में बढ़ते-बढ़ते अब 185 के करीब है। 1992 के आरंभ में सोवियत संघ के समाप्ति होने से उसके पूर्व स्वायत्त गणराज्य अब स्वतंत्र होकर इसके सदस्य बन गये हैं।
21. क्या गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है ?
Ans- नहीं, गुट निरपेक्षता को कभी भी नकारात्मक नीति की संज्ञा नहीं दी जा सकती है क्योंकि, दो विरोधी गुटों (पूँजीवादी एवं साम्यवादी) से अलग हटकर विकासशील देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का समाधान ढूंढने की बात सोची गई थी। उन दोनों में से किसी एक ग्रेट के सदस्य होने का मतलब ही था उसका गुलाम बनकर रहना। इसके अतिरिक्त गूट निरपेक्षता नीति का मुख्य उद्देश्य था शांति कायम करके अपने-अपने देशों का विकास करना जो सर्वथा उचित था। यदि यह नकारात्मक नीति होती तो आज शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी इसकी आवश्यकता एवं प्रसांगिकता नहीं होती। जो एक ऐतिहासिक सत्य है।
22. नाटो क्या है ?
Ans- उत्तरी अटलांटिक सन्धि संगठन (नाटो) का निर्माण 4 अप्रैल, 1949 को हुआ। इस सन्धि पर 12 देशों-अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नार्वे, पुर्तगाल, आइसलैण्ड तथा नीदरलैण्ड ने हस्ताक्षर किये। बाद में यूनान, टर्की, पश्चिमी जर्मनी, पोलैण्ड, हंगेरी, चैक गणराज्य को इसमें सम्मिलित कर लिया गया।
नाटो का निर्माण निम्न उद्देश्यों के लिये किया गया था-
1. सोवियत साम्यवाद को रोकना।
2. सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिये, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये यूरोपीय राष्ट्रों के लिये सुरक्षा छतरी प्रदान करना।
3. सोवियत संघ के साथ सम्भावित युद्ध के लिये लोगों को विशेषतया अमरीका के लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना।
23. पंचायती राज से आप क्या समझते हैं ?
Ans- पंचायती संस्थाओं का तात्पर्य ग्रामीण प्रशासनिक संस्थाओं से है। भारत में प्राचीनकाल से ही पंचायती संस्थाओं का अस्तित्व रहा है, क्योंकि भारत के ग्रामों के विकास के बिना देश की उन्नति असम्भव है और ग्रामों का विकास ‘ग्रामीण प्रशासन’ द्वारा ही सम्भव है। भारत में वैदिक काल में ग्राम प्रशासन का उत्तरदायित्व ग्राम पर ही था जो ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों की सहायता से काम करता था। सन् 1920 में संयुक्त प्रान्त, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में ग्रामीण उत्थान के लिए पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाये गये।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत 1952 में हुई जो 1992 में पुनः संशोधित किया गया।
24. सरपंच की शक्तियों का वर्णन करें।
Ans- पंचायत अधिनियम के अधीन दायर किया जाने वाला प्रत्येक वाद या मामला सरपंच के यहाँ दायर किया जाएगा और जहाँ सरपंच की सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो वहाँ उस सरपंच के यहाँ और ग्राम कचहरी की किसी न्याय पीठ द्वारा जिसमें सरपंच तथा वाद और मामले से सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा नामित किए जाने वाले ग्राम कचहरी के पंचों में से दो पंच और यथा विहित रीति से सरपंच द्वारा चुने गऐ दो अन्य पंच शामिल होंगे सुनवाई की जाएगी और उसका अवधारण किया जाएगा।
25. श्वेत क्रांति से क्या अभिप्राय है ?
Ans- आपरेशन फ्लड परियोजना देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गयी योजना है। यह योजना श्वेत क्रान्ति के नाम से भी जानी जाती है। यह योजना तीन चरणों 1970 से 1978, 1978 से 1985 तथा 1985 से 1994 में चलाई गयी थी। इस योजना के फलस्वरूप भारत में दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। दूध उत्पादन की वृद्धि के कारण इसे श्वेत क्रान्ति कहा जाता है। इस क्रान्ति से देश में दुग्ध उत्पादन, वितरण तथा उपभोग काफी बढ़ा है। इससे रोजगार में भी काफी वृद्धि हुई है।
26. पर्यावरण संरक्षण क्या है ?
Ans- वे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन कर देते हैं। वे पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। अतः पर्यावरण का संरक्षण नितांत आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण के मूलतत्व हैं वन, झील, नदी, पेड़-पौधों तथा पहाड़ों का संरक्षण। इसमें वन्य जीवन का संरक्षण एवं संवर्धन, शुद्ध पेय जल का संवर्धन इत्यादि आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्तव्य कहा गया है। भारत सरकार ने भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून बनाये हैं।
27. उत्तर दक्षिण संवाद का क्या हैं ?
Ans- हमारी पृथ्वी दो गोलाद्धों में विभक्त है-उत्तरी गोलार्द्ध तथा दक्षिणी गोलार्द्ध। उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप का क्षेत्र आता है। दक्षिण गोलार्द्ध में एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का क्षेत्र आता है। उत्तरी गोलार्द्ध में उन्नत, समृद्ध तथा विकसित देश हैं जबकि दक्षिणी गोलार्द्ध में निध ‘न पिछड़े तथा विकासशील देश अधिक हैं। दोनों तरह के देशों में कई बार विचार-विमर्श हुए तथा दोनों गोलाद्धों की स्थिति में समानता हेतु कई बार संवाद हुए जिसमें 1975 का पेरिस सम्मेलन प्रमुख है। इसके बाद 1986 से 1993 में गैट समझौते हुए लेकिन इन सम्मेलनों का दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा।
28. द्विध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता थी ?
Ans- द्विध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक नहीं हुआ बल्कि इसकी प्रासंगिकता बनी रही। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नव-स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था-दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता आज भी है।
29. सार्क क्या है ?
Ans- दक्षेस (साउथ एशियन एसोसियेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (SAARC) दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरूआत 1985 में हुई। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेस को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। दक्षेस के सदस्य देशों ने सन् 2002 में ‘दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार-क्षेत्र समझौते’ पर दस्तखत किये। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है।
30. भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं ?
Ans- एक लम्बे समय तक भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक दल अर्थात् कांग्रेस का प्रभुत्व रहा जिसका कारण प्रमुख रूप से यह था कि अन्य कोई दूसरा दल कांग्रेस के समान रूप में उभर कर नहीं आया। दूसरा कारण यह भी था कि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत साथ थी व पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गाँधी व सरदार पटेल लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों का नेतृत्व रहा। जिन्होंने देश को मजबूत किया बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। 1952 से लेकर 1967 तक 1971 से लेकर 1977 तक 1980 से लेकर 1989 तक 1991 से लेकर 1996 तक कांग्रेस का प्रभाव रहा है अर्थात् प्रभुत्व रहा है।
Political Science – राजनीतिशास्त्र | Class 12 ( Arts ) | By-Suraj Sir
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 31 से 38 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 5अंक निर्धारित है।
31. भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के पतन के मुख्य कारकों का परीक्षण करें।
Ans- देश का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि 1960 के दशक के अंतिम सालों में काँग्रेस के एक छत्र राज को चुनौती मिली थी। अतः काँग्रेस के पतन के निम्नलिखित कारण थे-
( i ) काँग्रेस पार्टी में आश्चर्यजनक नेतृत्व का अभाव – काँग्रेस के पतन का प्रमुख कारण काँग्रेस पार्टी के पास करिश्माई नेतृत्व का अभाव था क्योंकि 1964 में पंडित जवाहर लाल नेहरू का देहान्त होने के बाद काँग्रेस के नेतृत्व में एक प्रकार की शून्यता सी आ गयी थी।
(ii) काँग्रेस पार्टी के भीतर टूट- सिन्डीकेट और श्रीमती इन्दिरा गाँधी
के बीच मतभेद होने के कारण काँग्रेस में टूट हो गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप काँग्रेस पार्टी, काँग्रेस ई (काँग्रस इन्दिरा), काँग्रेस ओ इत्यादि पार्टियाँ बन गयी थीं।
(iii) काँग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद- राष्ट्रपति के चुनाव में काँग्रेस के
सिन्डीकेट वाली लॉबी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा किया और दूसरी तरफ श्रीमती गाँधी ने एक निर्दलीय के रूप में वी० वी० गिरी को खड़ा किया। वी० वी० गिरी राष्ट्रपति के चुनाव जीत गये। इस प्रकार के मतभेद काँग्रेस के पतन का कारण बना।
(iv) श्रीमती गाँधी की अपनी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शैली-
श्रीमती गाँधी स्वतंत्र होकर कार्य करती थी। सिन्डीकेट से कोई राय लेना आवश्यक नहीं समझती थी।
(v) काँग्रेस की आंतरिक गुटबाजी काँग्रेस के अन्दर बहुत सारे गुट बन गये जिन्होंने काँग्रेस को बहुत ही कमजोर बना दिया।
(vi) इन्दिरा गाँधी की लोकप्रियता बंगला देश की विजयोपरांत श्रीमती इन्दिरा गाँधी की लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी थी। इसी से मदहोश में आकर श्रीमती गाँधी ने आपातकाल लागू किया और परिणामस्वरूप काँग्रेस का पतन होने लगा।
(7) गैर-काँग्रेस पार्टियों का ध्रुवीकरण- आपातकाल के बाद काँग्रेस को शिकस्त देने के लिए सभी दलों ने एकजूट होकर जनता पार्टी बनायी और सन् 1977 के चुनाव में काँग्रस को हराया गया।
इस प्रकार उक्त कारणों के फलस्वरूप काँग्रस का पतन हुआ।
32. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए ?
Ans- सन् 1936 से पूर्व बिहार, उड़ीसा, आसाम एवं बंगाल के क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य था। 1936 में बिहार पृथक राज्य बना। पुर्नगठन अधिनियम के तहत 1956 में बिहार राज्य का पुर्नगठन हुआ। पुनः 2000 में वर्तमान झारखंड राज्य के क्षेत्र को बिहार से अलग कर बिहार का पुर्नगठन किया गया। अविभाजित बिहार खनिज सम्पदा में बहुत धनी था। लेकिन इन खनिज क्षेत्रों के झारखंड में चले जाने के कारण बिहार की ये सम्पदा लगभग नगण्य हो गई है। प्राचीन बिहार की सांस्कृतिक विरासत भी काफी संवृद्ध थी लेकिन वह भी आज नगण्य हो गई है। बिहार से झारखंड का विलगाव ने इसके औद्योगिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।
वर्तमान में बिहार मात्र एक कृषि प्रधान राज्य रह गया है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य ने वह प्रगति नहीं कर पायी है जो इसे करनी चाहिए थी। यहाँ के श्रमिक एवं किसान काफी मेहनती हैं। बिहार में जल संसाधन एवं कृषि योग्य भूमि की कमी नहीं है लेकिन कृषि में आधुनिक तकनीक का अभाव एवं व्यवहार की कमी से इसका समुचित विकास अभी तक नहीं हो पाया है।
आबादी की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साक्षरता के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी अन्य विकसित राज्यों की तुलना में काफी कम है।
किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की भारतीय संविधान में दो व्यवस्थायें हैं- पहला राजनीतिक एवं दूसरा आर्थिक। जम्मु-कश्मीर को संविधान के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि वहां बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक अशान्ति का भय है। बिहार को इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ आर्थिक संकट है। जम्मू-कश्मीर भारत के संघात्मक स्वरूप का दर्पण है इसलिए उस पर भारत का आधिपत्य बनाये रखने के लिए उसे विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, उन्हें अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। देश के 29 राज्य में ।। राज्यों को विशेष दर्जा मिला है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए सभी शर्तें बिहार के पास मौजूद हैं।
33. राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं ? राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है।
Ans- राष्ट्रपति शासन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन एक ऐसा शासन है जिसमें केन्द्रीय मंत्रिमण्डल भंग, हो जाती है और देश का शासन कार्य प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। राष्ट्रपति के नाम से देश का शासन कार्य चलाया जाता है। राष्ट्रपति शासन काल में राष्ट्रपति शक्तिशाली हो जाता है। वह संविधान के अनुसार देश में शासन कार्य चलाता है।
राष्ट्रपति शासन राज्य में भी उस समय लागू की जाती है जब राज्य की विधि व्यवस्था सही नहीं रहती है और राज्य मंत्रिमण्डल अपना इस्तीफा दे देता है तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लगाया जाता है जब किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए समुचित बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है और न ही किसी प्रकार की गंठबंधन सरकार का गठन होने की संभावना रहती है। राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होने से राज्यपाल ही उस राज्य का शासन कार्य चलाता है। लेकिन किसी भी राज्य में 6 माह से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रह सकता है।
अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को किसी राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी प्रकार से ज्ञात हो जाये कि ऐसी परिस्थिति हो गयी है कि राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। तब संसद द्वारा प्रस्ताव पास कर दो माह के भीतर स्वीकृत कराना आवश्यक होता है तब राज्य में 6 माह के लिये राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 44 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन एक वर्ष की अवधि तक रहेगा।
34. वित्त विधेयक क्या है ? वर्णन करें।
Ans- विधेयक दो प्रकार का होता है- (1) साधारण विधेयक (2) वित्त विधेयक।
साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में गैर-सरकारी या सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को पेश करने का अधिकार सिर्फ सरकारी सदस्य को ही प्राप्त है। इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। कौन विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद धन-विधेयक को भी उन सभी अवस्थाओं अर्थात् प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन से गुजरना पड़ता है जिससे साधारण विधेयक गुजरता है। धन-विधेयक को अस्वीकृत करने का अधिकार राज्य-सभा को प्राप्त नहीं है। दोनों सदनों द्वारा धन विधेयक पारित होने पर राष्ट्रपति को इस पर स्वीकृति देनी ही पड़ती है।
संविधान की 110वीं धारा में धन विधेयक की परिभाषा दी गयी है। कोई विधेयक धन विधेयक तभी समझा जायगा यदि उसका निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी एक विषय से सम्बन्ध हो-
(1) किसी टैक्स को लगाना, किसी टैक्स में वृद्धि करना या कोई परिवर्तन करना। (2) सरकार द्वारा ऋण लेने की व्यवस्था करना या आर्थिक. देनदारी लेना। (3) भारत के आकस्मिक फण्ड, संचित फण्ड के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करना। (4) भारत के संचित फण्ड में से किसी धनराशि को व्यय करना, (5) किसी सरकारी खर्च की भारत के संचित फण्ड पर डालना या इस फण्ड से खर्च किये जाने वाले धन की मात्रा में वृद्धि करना, (6) सरकार की वित्त विषयक देनदारियों के साथ सम्बन्ध रखने वाले कानून में संशोधन करना, (7) भारतीय संघ या उसके अन्तर्गत राज्यों के आय-व्यय के हिसाब की जाँच से सम्बन्ध रखने वाले विषय (8) वे संघ विषय जिनका सम्बन्ध ऊपर लिखी हुई बातों के साथ किसी और प्रकार से हो।
इस तरह वित्त सम्बन्धी विधेयक के तीन अंग हैं- (1) वार्षिक वित्त विवरण (2) अनुदान सम्बन्धी माँग और (3) विनियोग विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक।
1. वार्षिक वित्त विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में लोकसभा के समक्ष वार्षिक वित्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है।
2. अनुदान सम्बन्धी माँग: वार्षिक बजट के दूसरे भाग को अनुदान की माँग के रूप में संसद के समक्ष उपस्थित किया जाता है। इस अनुदान में कटौती का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
3. विनियोग विधयेक अनुदानों की मांग की स्वीकृति के बाद लोकसभा में भारत की संचित निधि से विनियोग के लिए विधेयक संसद में पेश किया जाता है। इसके स्वीकृत होने पर ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है।
35. एक प्रजातंत्र में सभ्य समाज की क्या भूमिका है ?
Ans- वर्तमान समय में प्रजातंत्र एक धर्म बन चुका है। यह सर्वमान्य धारणा है कि मानव शक्ति उन्मुख करने के लिए कोई भी व्यवस्था इतनी अधिक प्रबल नहीं है जितना कि प्रजातंत्र है। वर्तमान प्रजातंत्र राज्य प्रधान है। उसमें अनेक विचारधाराओं का मिश्रण हो गया है राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार प्रजातंत्र का सिद्धान्त अनेक सिद्धांतों व नियमों का समुच्चय है। यह न केवल वर्तमान ‘है’ से ही सम्बन्धित है वरन् अपने आदर्शों अर्थात् क्या होना चाहिए से भी सम्बन्धित है।
वास्तविक प्रजातंत्र उसी अवस्था में सफल कहलाता है जब समाज में सामाजिक समानता दिखलायी दे। वास्तविक प्रजातंत्र में रक्त लिंग व धर्म के आधार पर कोई भेद भाव नहीं होता। जिस समाज में ऊँच-नीच की भावना, – स्त्री-पुरूषों के अधिकारों में अंन्तर व धनी निर्धनों के मध्य भेद पाया जाता है वहाँ प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। प्रजातंत्र के लिए समाज में आर्थिक विषमता का अभाव भी आवश्यक है। धन का एकत्रीकरण कुछ व्यक्तियों के हाथ में न होकर उसका वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि सभी मनुष्यों को अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई का अनुभव न हो।
प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। उसे शासन में भाग लेने के लिए समान योग्यता का अधिकारी होना चाहिए। प्रजातंत्र में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी को वयस्कता के आधार पर मतं देने का और चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिलता है। प्रजातंत्र का लक्ष्य है सुरक्षा, न्याय, स्वतत्रंता, समानता व लोककल्याण, विकसित राज्य व्यवस्थाओं में प्रजातंत्र के ये ही लक्ष्य हैं। प्रजातंत्र कतिपय मान्यताओं पर कार्य करता है।
प्रजातंत्र में सभ्य समाज की भूमिका इस प्रकार है-
(i) देश निर्माण के लिए सदैव सहयोग प्रदान करना चाहिए।
(ii) निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पादित कराने में सहयोग।
(iii) शांति व्यवस्था स्थापित कर समाज का विकास।
(iv) राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के प्रति जबावदेही।
(v) शांति पूर्वक विरोध प्रदर्शन।
36. सांप्रदायिकता क्या है ? भारतीय राजनीति पर इसके प्रभावों की विवेचना करें।
Ans- भारत में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि अनेक धमों। के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म में अनेक संप्रदाय पाएं जाते हैं। एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों पर विश्वास नहीं है। इसी को संप्रदायिकता कहा जाता है। वैसे संप्रदायिकता का पर्याय ‘हिन्दुत्व’ से भी लगाया जाता है। इस ‘हिन्दुत्व’ शब्द का प्रतिपादक सावरकर थे जिनका कहना था कि भारत हिन्दुओं का देश है, हिन्दू वही है जो इस देश को अपनी मातृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। अतः जो ऐसा नहीं करता है, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता के निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं :
(1) साम्प्रदायिकता ने लोकतंत्र को कमजोर किया है क्योंकि मतदान का आधार कई क्षेत्रों में धार्मिक पहचान बन गयी है तथा वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हट गया है।
. (2) राजनीति में साम्प्रदायिकता के समावेश से धार्मिक समुदायों में तनाव, रंगों और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी है।
(3) साम्प्रदायिकता के कारण राजनीतिक लाभ की दृष्टि से राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टीकरण और वोट की नीति अपना ली है जबकि उनका वास्तविक विकास नहीं हो पाया है।
(4) साम्प्रदायिकता के कारण राजनीतिक दलों का विभाजन साम्प्रदायिकता के आधार पर हो जाता है तथा राजनीतिक दलों में विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर मतैक्य का निर्माण नहीं हो पाता है। भारतीय राजनीति में अधिकांश दल भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक दल घोषित कर आपसी आरोप प्रत्यारोप में संलग्न रहते हैं। ऐसी स्थिति देश के विकास के लिए हानिकारक है।
(5) सांप्रदायिकता की तीव्र भावना राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर खतरा है। वर्तमान में आतंकवाद का मुद्दा भी कहीं न कहीं संप्रदायिकता से जुड़ा है।
इस प्रकार संप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को बहुत ही प्रदूषित एवं-विषाक्त कर दिया है।
37. वर्ष 2000 से भारत अमेरिका संबंधों का परीक्षण कीजिए।
Ans- 1999 से अमेरिका ने भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला है. और दोनों देशों के आपसी संबंधों में सुधार हुआ हे। सितंबर 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकवादी आक्रमण के बाद तो भारत-अमेरिकन संबंध काफी मधुर तथा सहयोगी हुए हैं। 1999 में कारगिल युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी सेनाएँ भारतीय सीमा से वापस ले जाने को कहा और भारत का समर्थन किया।
आज अमेरिका भारत के साथ कई विषयों पर सहयोग विशेषकर सूचना तकनीक पर, परस्पर सहायता और मित्रता के संबंध बनाए हुए हैं। सन् 2001 की दीपावली के अवसर पर अमेरिकन व्हाइट हाउस पर रोशनी करके अमेरिका ने भारत-अमेरिका मैत्री को गूढ़ स्वरूप देने का प्रयत्न किया है। परन्तु विश्व भर से आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लेने के बाद भी वह पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियाँ रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है।
आज यह बात भी निश्चित है कि अमेरिका और भारत एक-दूसरे के काफी समीप आ चुके हैं। अमेरिका जानता है कि आतंकवाद की समाप्ति के प्रयास में भारत अमेरिका के लिए प्रभावकारी शक्ति सिद्ध हो सकता है और भारत तथा अमेरिका के बीच व्यापार तथा तकनीक के आदान-प्रदान के काफी अवसर विद्यमान हैं। अमेरिका ईराक में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेनाओं को भेजे जाने के लिए दबाव डालता रहा है। परंतु भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बिना वहाँ अपनी सेनाएँ भेजने से इंकार कर दिया।
2006 में प्रथम मार्च से तीन मार्च अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने भारत की यात्रा की। अन्य समझौतों के साथ ही भारत के साथ एक अणु संधि की जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता हैं इसके अंतर्गत अमेरिका ने भारत को अणुशक्ति के रूप में स्वीकार किया और भारत को शांति तथा विकास के उद्देश्यों में प्रयोग किए जाने के लिए यूरेनियम की आपूर्ति करने का वचन दिया। बेशक अमेरिकन कांग्रेस ने उसमें कुछ संशोधन किए हैं, फिर भी यह संधि बड़ी महत्वपूर्ण है और भारत-अमेरिका संबंधों को दृढ़ बनाने वाली है।
भारत ने विश्व राजनीति में गुटबंदी में सम्मिलित न होकर अपना ध्यान अपने सामाजिक-आर्थिक विकास की ओर केन्द्रित रखा है। भारत ने आर्थिक वृद्धि-दर को प्राप्त करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी में भी प्रगति की है। इन बातों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत से गूढ़ संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया है। अमेरिका में बसे भारतवासियों ने भी यह साबित किया है कि भारतीयों में आगे बढ़ने की क्षमता तथा उत्साह है।
38. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकार का परीक्षण करें।
Ans- संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायधीश तथा जब तक संसद कानून द्वारा इस संख्या को बढ़ा नहीं दे, अधिक से अधिक सात अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। संसद इस संख्या को घटा नहीं सकती, उसे केवल ‘बढ़ाने का अधिकार है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के कानून 1956 ई० के द्वारा संसद के अन्य न्यायाधीशों की संख्या अधिक से अधिक दस कर दी थी। 1960 ई० में संसद से एक दूसरा कानून बनाकर इस संख्या को तेरह कर दिया। अब मुख्य न्यायाधीश के सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 16 हो गयी है।
अध्ययन के दृष्टिकोण से इसके क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। यथा-
1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार : इस न्यायालय को ऐसे मुकदमों पर प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है जो ‘भारत सरकार तथा दूसरे राज्यों की सरकारों के बीच, अथवा दो या दो से अधिक राज्यों की सरकारों के संवैधानिक विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न हो।
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार : उच्चतम न्यायालय को राज्यों के उच्च न्यायालय से तीन प्रकार की अपीलें सुनने का अधिकार प्राप्त हैं :-
(क) संवैधानिक : इसे संवैधानिक विवादों को सुनने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार की अपील उसी समय सुनी जायगी जब की किसी राज्य का उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे दे कि इस विवाद के मूल में संविधान की व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न है। यदि उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र नहीं देता है तो न्यायालय को अधिकार है कि वह स्वयं उसका प्रमाण-पत्र दे दे।
(ख) दीवानी : दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील निम्नलिखित अवस्थाओं में की जा सकती है-
(i) यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद का मूल्यः बीस हजार रु० से कम नहीं है, परन्तु अब भारतीय संविधान संशोधन (1976) के अनुसार यह बीस हजार रु० की सीमा बन्दी हटा दी गई है। अथवा
(ii) मामला अपील के योग्य है।
(iii) उच्च न्यायालय स्वयं भी फौजी अदालतों को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय के विरूद्ध करने की विशेष अनुमति दे सकता है।
(ग) फौजदारी : फौजदारी सम्बन्धी मामलों की अपील की जा सकती है। इसमें सम्बन्धित विवादों की अपील उसी समय होगी जब कि उच्च न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति को मृत्यु दंण्ड की आज्ञा में परिवर्तित कर दिया हो या उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाण-पत्र दे दे कि यह मामला उच्चता यायालय में अपील करने योग्य है।
3. परामर्श का क्षेत्राधिकार : उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को समय-समय पर परामर्श भी देता है। राष्ट्रपति जब चाहे, – महत्वपूर्ण, वैधानिक मामलों, समझौतों, संधियों या पुरानी रियासतों के साथ संधियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है।
4. आवृति सम्बन्धित क्षेत्राधिकार : उच्चतम न्यायालय को अपने दिये गये निर्णय या आदेश पर पुनर्विलोकन का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संविधान की धारा 32 के अधिन विभिन्न प्रकार के लेखों को जारी करने का अधिकार प्राप्त रहने के कारण भी यह देश के किसी भी न्यायालय के निर्णय को दुहरा सकता है।
5. निरीक्षण तथा प्रशासकीय अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय को कुछ महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय अधिकार भी प्राप्त है। यह अपने उत्तरदायित्व को ठीक से चलाने के लिए अपने संबंध में स्वयं नियमों का निर्माण कर सकता है। इस न्यायालय के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को है। इसके लिए उसे राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ती है।
यदि आपको यह मॉडल पेपर पसंद आया हो तो इसे लाइक , कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ” धन्यवाद “
Important Links
| My Official Website | Visit Now |
|---|---|
| Youtube Channel | Click Here |
| Whatsapp Channel | Click Here |
| Telegram Channel | Click Here |
| Instagram Id | Click Here |