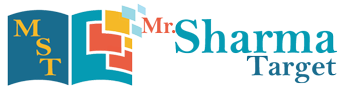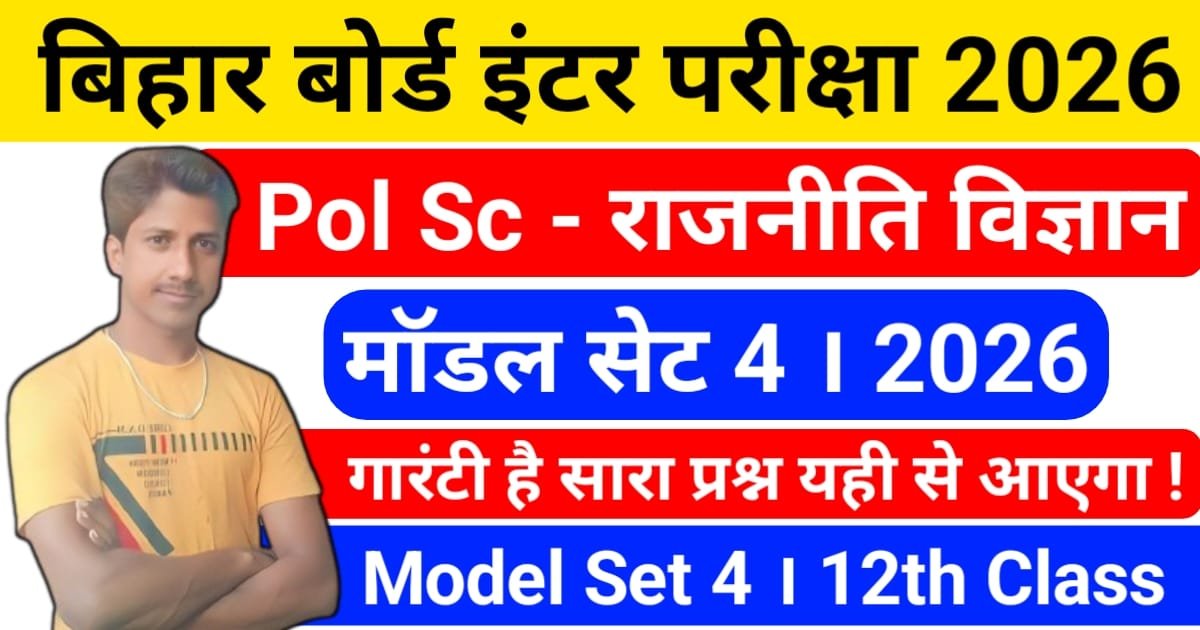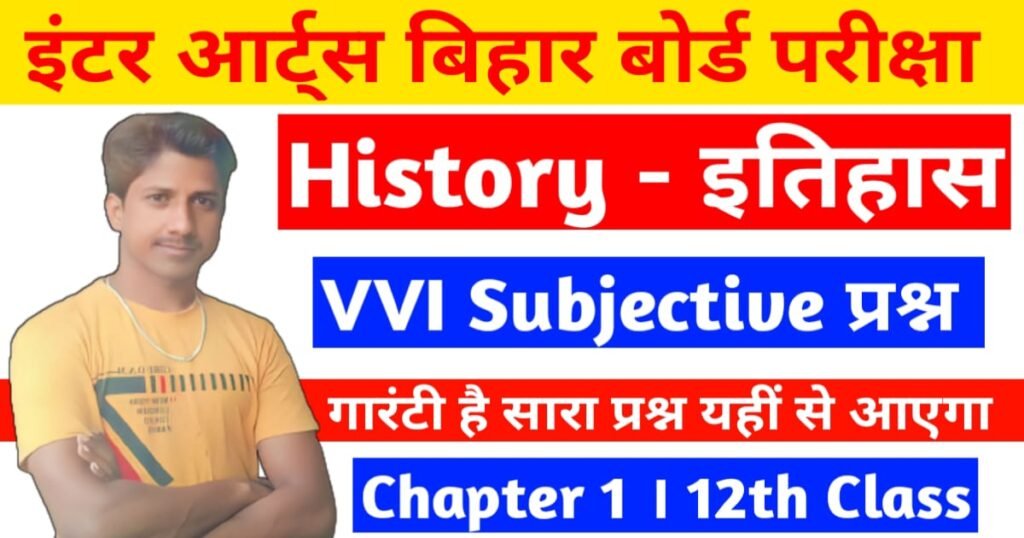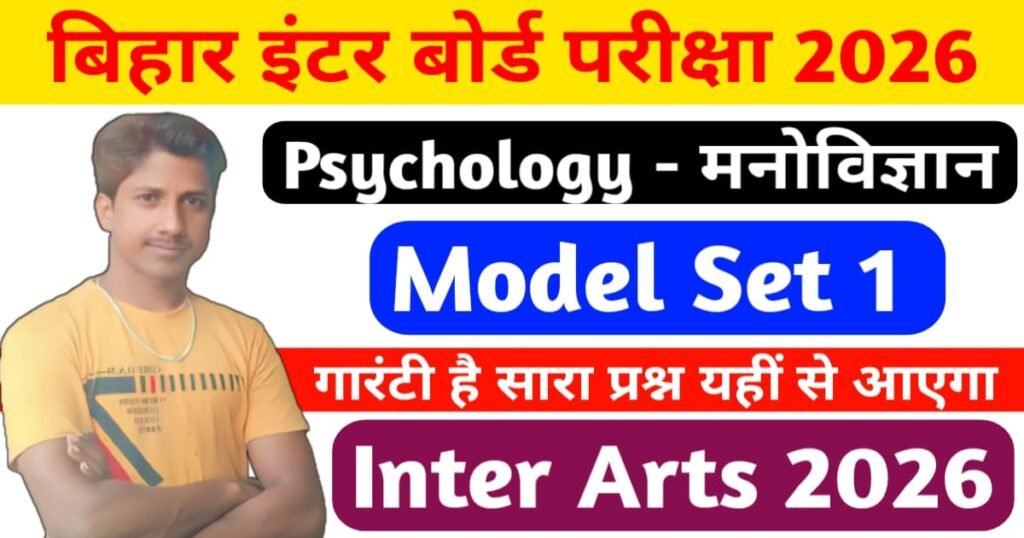Bihar Board 12th Class Political Science Model Set 4 Subjective – Answer
यदि आप बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप शामिल होने वाले हैं तो यह पोस्ट आपके लिए ही है इस पोस्ट में हम आपको राजनीतिशास्त्र का मॉडल सेट 4 लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आसान भाषा में प्रश्न और उत्तर करने वाले हैं। यदि आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में राजनीतिशास्त्र में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस पोस्ट में जितने भी क्वेश्चन लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन किया जा रहा है। सभी प्रश्न को अच्छे से कमांड कर लीजिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्न इसी मॉडल सेट से आने वाले हैं।
| Subject | Political Science - राजनीतिशास्त्र |
|---|---|
| Class | 12th |
| Model Set | 4 |
| Session | 2024-26 |
| Subjective Question | All Most VVI Questions |
Political Science – राजनीतिशास्त्र | Class 12 ( Arts ) | By-Suraj Sir
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही 15 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए दो अंक निर्धारित है।
1. एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है ?
Ans – साधारणतः देखा जाता है कि बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें कई तरह के पार्टियाँ होती है किन्तु किसी एक ही पार्टी या कई पाटियों के समूह के पास सता होती है। शेष पार्टियाँ सता में भागीदारी नहीं कर सकती है। जैसे-स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी के ही सत्ता रही। उसे 1952 के पहले 1957 के दूसरे व 1967 के तीसरे आम चुनावों में विशाल बहुमत मिला। अन्य पार्टियाँ इतनी कमजोर थी कि वे कांग्रेस से प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकते थे।
2. भारतीय प्रधानमंत्री के किन्ही चार अधिकारों को लिखें।
Ans – भारतीय प्रधानमंत्री को ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।
(i) मंत्रिपरिषद् का निर्माण – प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का निर्माण करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद् के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
(ii) विभागों का बँटवारा – प्रधानमंत्री केवल मंत्रिपरिषद का निर्माण ही नहीं करता बल्कि मंत्रियों के बीच विभागों का बँटवारा भी करता है।
(iii) मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना – प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता भी करता है, मंत्रिमंडल की बैठक की रूपरेखा तय करता है।
(iv) मंत्रियों के बीच के विवादों को मिटाना – प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों के बीच उत्पन्न विवादों एवं मतभेदों को दूर करता है और मंत्रियों के बीच समन्वय बनाए रखने का काम करता है ताकि सरकार का काम सुचारू रूप से चल सके।
3. क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं ?
Ans – क्षेत्रीय दल भारत की राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है और यह भारत के लिए एक जटिल समस्या बनी रही है और आज भी विद्यमान है। क्षेत्रीय दल किसी खास क्षेत्र को ज्यादा महत्त्व देती है। इसके सिद्धांत एवं नीतियाँ किसी विशेष क्षेत्र एवं वर्ग तक सीमित रहती है।
4. वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को बताएं।
Ans – वैश्वीकरण विश्व को सकारात्मक ढंग से प्रभावित किया। इसने राज्यों को विश्व व्यापार में नियंत्रण की समस्या से मुक्त कर दिया है। इससे लोगों को भी विश्वव्यापी सामान तथा तकनीकी उपलब्ध हो रहे हैं। व्यापार में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है, जिससे उत्तम कोटि की सामानों के व्यापार में लाभ मिला है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लोगों को रोजगार पाने तथा व्यापार करने की अपार संभावनाएँ देखने को मिलती है। विकास तथा क्षमता प्रदर्शन के नये अवसर उपलब्ध हुए हैं। इससे हर देश का विकास हुआ है, भारत इसका लाभ काफी अधिक उठा रहा है। वैश्वीकरण उदारवाद एवं खुलेपन की नीति पर आधारित है। इस प्रकार वैश्वीकरण ने अब तक सुरक्षा की समस्या से चिंतित विश्व को विकास, व्यापार, सहयोग तथा समन्वय का नया आयाम दिया है।
5. भूमंडलीय तापन क्या है ?
Ans – जब कभी धरती के तापमान में वृद्धि होती है, अनेक समस्याएँ उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोक्साइड में वृद्धि के कारण ताप बढ़ता है, बर्फ पिघल सकता है तथा प्रलय की संभावना को नजदीक लाता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षक आवश्यक है। इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेज तथा असंतुलित रूप से प्राकृतिक के संसाधनों का दोहन करना ही जिम्मेवार है।
6. भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है ?
Ans – भारत में चुनावी प्रक्रिया संपन्न करने के लिए भारतीय संविधान में एक सदस्यीय चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है जिसका प्रमुख उत्तरदायित्व या कार्य विभिन्न स्तर पर स्वतंत्र रूप से या शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना है। इस समय चुनाव आयोग तीन सदस्यीय है। जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है व दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं।
7. ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका से आप क्या समझते हैं ?
Ans – मार्च 1985 में सोवियत संघ में गोर्वाचोब का नेतृत्व स्थापित हुआ। उन्होंने अपना नया सोच प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता बहाल की तथा अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण किया। ग्लासनोस्त का अर्थ है समाज को खोलो। पेरेस्त्रोइका का अर्थ है आर्थिक नव-निर्माण करो। इस प्रकार लेनिन के समय से चली आ रही वह व्यवस्था समाप्त हुई जिससे लोगों को मूक व वधिर पशुओं की तरह बना दिया गया था तथा निजी अर्थव्यवस्था पूर्णतया उन्मूलित की गई थी। गोर्बाचोव की दृष्टि में गिरते हुए समाजवादी राज्य को बचाने का यही रास्ता था।
8. सार्क के उद्देश्य बताएं।
Ans – दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन (SAARC) के चार्टर के अनुच्छेद 1 में सार्क के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है-
(i) दक्षिण एशिया के देशों की जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।
(ii) दक्षिण एशियाई देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता का विकास करना।
(iii) इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास की गति तेज करना।
9. मौलिक अधिकार का वर्णन करें।
Ans – भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को छः प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं-
(i) समानता का अधिकार
(ii) स्वतंत्रता का अधिकार
(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(v) सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार
(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
10. मैक मोहन रेखा क्या है ?
Ans – भारत एवं चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ई० में शिमला में निर्धारित की गयी थी। इसकी उतरी पूर्वी सीमा की लंबाई 4224 किमी० है।
11. अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है ?
Ans – अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। प्रजातंत्र को आमतौर पर एक शासनतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में प्रजातंत्र सरकार का एक संगठन है, जो जनता द्वारा निर्मित, नियंत्रित एवं संचालित होता है। प्रजातंत्र राज्य के रूप में वह व्यवस्था है जिसमें सम्प्रभुता जनता में निवास करती है। शासन व्यवस्था का अंतिम अधिकार एवं निर्णय जनता के हाथ में रहता है। इसलिए हर्नशा ने कहा है कि इसमें राज्य का समस्त जन समूह सम्प्रभुता का अधिकारी होता है।
12. सामूहिक सुरक्षा क्या है ?
Ans – सामूहिक सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति प्रबन्धन का आधुनिक साधन है तथा राज्यों की पारस्परिक सुरक्षा की व्यापक अवधारणा है। इसके अन्तर्गत राज्यों के बीच एक पारस्परिक आवश्यक समझौता है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी देता है और शायद इसी गारंटी की वजह से दूसरे राष्ट्रों द्वारा किये वायदों द्वारा उसे अपने सुरक्षा की गारंटी मिलती है। सामूहिक सुरक्षा में मानव अस्तित्व और देश की खतरे से मुक्ति मिलती है।
13. चिपको आंदोलन के प्रभाव को लिखें।
Ans – 1973 में वन विभाग के ठेकेदारों ने जंगलों में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी। वनों को इस तरह कटते देख किसानों ने बड़ी संख्या में इसका विरोध किया और चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। स्पष्ट है कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन है। चिपको आंदोलन के द्वारा लोग पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए इसे चारो तरफ से घेर कर पेड़ से चिपक जाते हैं। इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा-
(i) चिपको आंदोलन से उत्तराखण्ड में वन संरक्षण के लिए लोगों में नवीन उत्साह का संचार मिला।
(ii) ‘चिपको आंदोलन केन्द्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया गया।
(iii) इस आंदोलन से लोगों को वनों से होने वाले आर्थिक कमाई सुरक्षित रह गई एवं लोगों के न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण हो गया।
(iv) चिपको आंदोलन लोगों को वनों के प्रति उदासीनता को खत्म कर दिया।
(v) इस आंदोलन से महिलाओं को जागरूक किया और महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
14. शिक्षा रोजगार में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति का अंतर बताएं।
Ans – पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अंतर है। स्त्री साक्षरता 2001 में 54.16 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों की साक्षरता 75.85 प्रतिशत थी। शिक्षा के अभाव के कारण रोजगार, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता सीमित हैं।
15. अयोध्या विवाद से आप क्या समझते हैं ?
Ans – अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है। जो नब्बे के दसक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्म भूमि और वाबरी मस्जिद को लेकर हैं। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिन्दू मंदिर को ध्वस्त कर वहाँ मस्जिद बनाया गया था। मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद को एक राजनैतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया, जो 6 दिसम्बर, 1992 को एक दंगे में बदल गया। यह विवाद राजनैतिक होते हुए कानूनी रूप में बदल गया। जिसे 9 नवम्बर, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद पटाक्षेप माना गया।
16. लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य हैं ?
Ans – लोकसभा में जो दल सरकार में शामिल नहीं होती है। वह दल विपक्षी दल कहलाते हैं। विपक्षी दलों के एक नेता का चुनाव किया जाता है, जिसे विपक्ष के नेता कहा जाता है। विपक्ष के नेता के प्रमुख कार्य हैं- सरकार की नीतियों की खामियाँ निकालना और उसकी अलोचना करना। हमेशा एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहना। विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर लोकसभा का बहिष्कार कर आदि माध्यमों के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को रचनात्मक सहयोग भी प्रदान करती है।
17. 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
Ans – राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवदेन के आधार पर भारतीय संसद ने 31 अगस्त, 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इसे 1 नवम्बर, – 1956 से लागू किया गया। इस अधिनियम संघ की इकाइयों की संख्या 28 से घटाकर 20 कर दिया। इसके द्वारा भारतीय क्षेत्र दो प्रकार की इकाइयों में विभाजित किया-एक, राज्य इकाई तथा दूसरा केंद्रशासित क्षेत्र। इस अधि नियम के द्वारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को 5 मंडलों में विभाजित किया गया। जिनके लिए अलग-अलग मण्डलीय परिषद् की स्थापना की गई। इस अधि नियम के द्वारा राज्यों की विधानपरिषद् की संख्या निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में भी परिवर्तन किया गया।
18. 1956 के बाद नए राज्यों के निर्माण का उल्लेख करें।
Ans – 1956 के बाद भारत में क्षेत्रीयता, भाषा, नस्ल एवं संस्कृति के आधार पर बहुत से नये राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे 1960 के बाद बम्बई से कटकर गुजरात एवं आसाम से कटकर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों का निर्माण हुआ। बाद में चलकर सन् 2000 में झारखण्ड, उत्तरांचल एवं छत्तीसगढ़ राज्य बने।
19. भारतीय संघ में हैदराबाद के विलय का विवरण दीजिए।
Ans – हैदराबाद के शासक को ‘निजाम’ कहा जाता था। वह हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा चाहता था। जिसके कारण लोगों ने शासन के विरुद्ध आंदोलन ने जोर पकड़ा। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ सैनिक बल का प्रयोग किया। निजाम के दमनकारी नीतियों के कारण भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुँची। कुछ रोज तक रुक-रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया।
20. भारत में नियोजन से आप क्या समझते हैं ?
Ans – नियोजित आर्थिक विकास का अर्थ है- आर्थिक विकास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ इस प्रकार से की जाये जिनसे निश्चित अवधि में निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके तथा जिससे उपलब्ध स्त्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग व उपयोग करके उत्तम परिणाम प्राप्त किया जा सके।
21. लोक अदालत क्या है ?
Ans – भारत में न्याय व्यवस्था को सुलभ, सुगम एवं त्वरित न्याय के लिए न्याय का एक अन्य मार्ग निकाला गया है जिसे लोक अदालत कहा गया है। लोकअदालत का अर्थ है लोगों का अदालत या न्यायालय। इस न्यायालय में विवादों का आपसी सहमति से निपटाया जाता है। लोक अदालत में विवादों का निपटारा सभी स्तरों पर सर्वोच्च न्यायालय का स्तर, उच्च न्यायालय का स्तर जिला न्यायालय का स्तर पर आपसी सहमति से निपटाने के लिए गठित की जाती है।
22. पीली क्रांति क्या है ?
Ans – तेलहन की फसल में अभूतपूर्व उत्पादन लक्ष्य रखने हेतु इसे पीली क्रांति नाम दिया गया। भारत तेल उत्पादन मामले में आत्मनिर्भर हुआ है। यहाँ तेलहनी पौधों के अच्छी उपज के लिए विशेष रुप में किसानों को अच्छी बीज के साथ-साथ उसमें उपयुक्त होने वाली कीटनाशक दवाओं की भी मुख्य रूप से उपलब्धता पर ध्यान दिया गया है। यहाँ तेलहनी पौधों में मुख्यतः सरसों, तीसी, राई, कुसुम, सूर्यमुखी आदि अनेक हैं जिसमें से तेल को निकाला जाता है।
23. भारत के किसी एक सामाजिक आंदोलन का उल्लेख करें।
Ans – एक सामाजिक आंदोलन के रूप में आंध्रप्रदेश के नेल्लौर जिले के एक दूरदराज के गाँव दुबरगंटा में महिलाओं द्वारा चलाये गये शराब विरोधी आंदोलन का उल्लेख किया जा सकता है।
1990 के प्रारंभिक दौर में यहाँ महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने पंजीकरण कराया। महिलाओं ने शिक्षण स्थल पर घर के पुरुषों द्वारा देशी शराब पीने, ताड़ी पीने तथा इस कारण आर्थिक दबाव में रहने एवं महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का बर्ताव करने की चर्चाएँ होने लगी। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं ने संगठित होकर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। यह एक उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार महिलाओं ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से इतनी जागरूकता प्राप्त की कि वे शराब विरोधी आंदोलन के लिए लामबंद हुई। शराब विरोधी आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से महिलाएँ संगठित होकर शराव बिक्री, घरेलू हिंसा आदि का विरोध किया। बाद में दहेज प्रथा, सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न, महिला प्रतिनिधित्व आदि मुद्दे इस आंदोलन का हिस्सा बन गया।
24. राज्यों के स्वायतता आप क्या समझते हैं ?
Ans – राज्यों की स्वायतता का अर्थ है, राज्यों को अधिकाधिक स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करना। भारत में स्वायतता की मांग सबसे पहले पंजाब प्रांत से उठी। 1970 के दशक में अकालियों ने पंजाब को और स्वायतता की मांग की। इस आशय का प्रस्ताव 1973 में आनंदपुर साहब में हुए सम्मेलन में पारित किया गया। ऐसे तो राजनीतिक स्वायतता की मांग आजादी के बाद से ही शुरू हो गया। जिसकी झलक आसाम में देखने को मिलती है। जहाँ गैर आसामी लोग असमी भाषा को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया वही जनजातीय समुदाय के लोग असम से अलग होना चाहते हैं।
दरअसल स्वायत्तता की मांग संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है तो राष्ट्रहित माना जाता है। जबकि कुछ समुदायों ने स्वायत्तता की मांग संविधान एवं देश के खिलाफ मांगकर अलगाव का जन्म दिया है।
25. पंचवर्षीय योजना क्या है ?
Ans – पंचवर्षीय योजना द्वारा विचार किए गए विकास के नमूने की प्रमुख विशेषताओं का मुख्य उद्देश्य पोषणकारी आर्थिक विकास के लिए एक स्वस्थ बुनियाद प्रदान करना, लाभदायक रोजगार के लिए बढ़ते हुए अवसर तथा जनता के लिए जीवन स्तर तथा श्रम की शर्तों को सुधारना है।
पंचवर्षीय योजनाएँ व्यक्तिगत पहल, सहकारी तथा संयुक्त प्रयत्नों के विषय क्षेत्र को विस्तृत करती है। आर्थिक तत्व को अवश्य ही अधिक महत्त्व देना होगा, परंतु सामाजिक क्षेत्र के कुछ पहलुओं की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना विकास की एक कड़ी है।
26. योजना अवकाश क्या है ?
Ans – तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) के बाद क्रम में व्यवधान पड़ गया। इसलिए एकवर्षीय योजनाएँ बनीं जिन्होंने 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 की अवधि को लिया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। तीन वर्षों की अवधि में तीन वार्षिक योजनाएँ आयीं। पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम ही टूट गया। इसी को योजना अवकाश का नाम दिया गया।
27. बीमारू राज्यों का क्या अर्थ है ?
Ans – वह राज्य जहाँ खनिज संपदा नगन्य हो, कृषि, सिंचाई, कल कारखाने, सड़क, बिजली, अस्पतालों, स्कूल तथा कॉलेजों की कमी के कारण बच्चों को सही शिक्षा न मिल पाना तथा राज्य के जनता को पेट भरने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर करना पड़े। शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़े। जिसके कारण अभिभावकों को अधिक खर्च करना पड़े, इन सारी कमियों के कारण ऐसे राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है।
28. योजना आयोग पर टिप्पणी लिखें।
Ans – योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, 1950 को केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया। आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके दैनिक कार्य का सम्पादन उपाध्यक्ष करता है। केन्द्रीय वित्त मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इसकी सिफारिशें तभी लागू होती हैं जब केन्द्रिय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया जाता है। आयोग के चार प्रमुख प्रभाग हैं जिनके माध्यम से आयोग कार्य करता है।
(i) समन्वय प्रभाग (ii) सामान्य प्रभाग (iii) विषय प्रभाग (iv) विशिष्ट प्रभाग।
राष्ट्रीय विकास को सुनिश्चित करना एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु बैठक आयोजित करना आयोग का मूल कार्य है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास परिषद व राष्ट्रीय आयोजन परिषद भी योजनाएँ तैयार करने में सहायता करती हैं।
29. ताशकंद समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Ans – ताशकंद समझौते (Taskand Agreement)- भारत और पाक के 1965 के युद्ध के बाद दोनों के बीच एक संधि हुई है जिसे ताशकंद समझौता कहा गया। ताशकंद समझौता सोवियत संघ के प्रभाव से हुआ था। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ के हस्ताक्षर हुए और उसी 11 जनवरी, 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुकने से निधन हो गया।
30. सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार क्या है ?
Ans – वीटो, लैटिक शब्द का अर्थ है- “मैं निषेध करता हूँ”। सुरक्षा परिषद में इसके स्थाई सदस्य अमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस, रूस तथा चाइना है। इसमें से कोई सदस्य सुरक्षा परिषद् के किसी प्रस्ताव पर ‘वीटो’ कर सकता है। यानी रोक सकता है।
Political Science – राजनीतिशास्त्र | Class 12 ( Arts ) | By-Suraj Sir
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 31 से 38 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्ही 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 5अंक निर्धारित है।
31. किसी राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या करें।
Ans – भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र में जो स्थिति प्रधानमंत्री का होता है लगभग वही स्थिति राज्य की शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री की भी है। मुख्यमंत्री राज्य की शासन की धुरी है। उसके कार्य एवं अधिकार काफी व्यापक है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रीपरिषद् का निर्माण करता है और मंत्रियों के बीच विभागों का बँटवारा भी करता है। मुख्यमंत्री सभी विभागों के कार्यों में समन्वय बनाए रखने का काम करता है ताकि सरकार का काम सुचारु रूप से चलता रहे। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। वह राज्य विधानमंडल का नेता भी होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने कार्य दायित्वों में निपटारा हेतु परामर्श भी देता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल बड़े-बड़े पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ एवं सजायाप्ता कैदी को क्षमादान भी प्रदान करता है। नीति निर्धारण में मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व एवं अपने दल के चुनावी घोषणा एवं सिद्धांत का प्रभाव देखा जा सकता है। राज्यपाल द्वारा जिला जजों की नियुक्ति एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से ही किया जाता है। मुख्यमंत्री की इच्छानुसार संचालित होता है। वह राज्य शासन का कप्तान होता है। राज्य में आए विशिष्ट अतिथियों का राज्य की ओर से स्वागत करता है।
32. राजनीतिक न्याय क्या है। वर्णन करें।
Ans – राजनीति न्याय का अर्थ है कि राज्य की राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया में किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं हो और सबको उसमें भाग लेने की स्वतंत्रता एवं समान अवसर प्राप्त हो। इस कारण लोकतंत्र राजनीतिक न्याय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है और अधिनायकवाद को राजनीतिक न्यायं का विलोम कहा जाता है। राजनीतिक न्याय के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं-
(i) शासनप्रणाली का प्रतिनिधिमूलक होना
(ii) सब वयस्कों को मताधिकार प्राप्त होना
( iii) नियमानुसार निष्पक्ष चुनाव होना
(iv) चुनावों में सभी नागरिकों को प्रत्याशी बनाने का अधिकार होना
(v) राज्य के सर्वाधिक पदों पर सभी नागरिकों को चुने जाने, नियुक्त होने का समान अवसर प्राप्त होना। कुछ अन्य अधिकार जो राजनीतिक न्याय को स्पष्ट करते हैं इस प्रकार हैं-
- राजनीति दल गठित करने का अधिकार
- भाषण एवं अभिव्यक्ति (प्रेस) की स्वतंत्रता
- सभाएँ अथवा मीटिंग करने की स्वतंत्रता
- संघ या संवाद बनाने की स्वतंत्रता
- प्रचार करने की स्वतंत्रता ।
- संक्षेपतः राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रक्रिया में भाग लेने की समान स्वतंत्रता को ही राजनीतिक न्याय कहा जाता है।
33. भारत में राज्यों के पुनर्गठन का विवेचना कीजिए।
Ans – भारत के सामने राज्यों का पुनर्गठन सबसे बड़ी चुनौती थी। उस समय भारतवर्ष छोटे-छोटे नरेशों के राज्यों में बँटा हुआ था। 567 देशी राज्य भारतीय एकता के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। 3 जून की घोषणा ने यह निश्चित किया कि अगस्त 15, 1947 को सभी स्थानीय राज्य भी स्वतंत्र हो जाएँगे। इन राज्यों को यह अधिकार था कि वे अपनी मर्जी से भारत यां पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएँ या उन्हें स्वतंत्र रहने का भी अधिकार था। यह पसंद भारतीय अखण्डता और एकता के लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि यह अनेक राज्य भारतीय भू-क्षेत्र में बिखरे हुए थे और अगर वे स्वतंत्र रह जाने के लिए ठान लेते तो अवश्य ही भारत की एकता व अखण्डता नष्ट हो गई होती। सरदार पटेल तथा उनके विश्वसनीय मित्र, विदेश विभाग के सचिव वी० पी० मेनन ने बड़ी सूझ-बूझ के साथ स्थिति को सँभाला। उन्होंने अनेक राजाओं के साथ वार्तालाप करने हेतु सामाजिक बैठक और अनौपचारिक पास-पड़ोस को चुना, भोजन तथा चाय पर दिल्ली अपने आवास पर आमंत्रित किया। पटेल राजाओं को यह विश्वास दिलाते थे कि कांग्रेस तथा राजसी व्यवस्था में कोई टकराव नहीं है। पटेल ने राजाओं के विचारों को भी सुना और उनकी जो धारणाएँ थीं उनकी तरफ भी ध्यान दिया। पटेल ने भारतीय नरेशों का देश-भक्ति के लिए आह्वान किया और चाहा कि वे उनके राष्ट्र की स्वतंत्रता में शामिल हों और ऐसे उत्तरदायी शासकों के रूप में व्यवहार करें जिन्हें अपने लोगों के भविष्य के बारे में चिन्ता है।
34. राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य है ?
Ans – भारत में आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग (नीति आयोग) के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थापना 6 अगस्त, 1952 को किया गया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य नीति आयोग (योजना आयोग) का है और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित होती है। इन्हीं सब कारणों से यह सर्वोपरि कैबिनेट (Super Cabinet) की ख्याती प्राप्त कर ली है। राष्ट्रीय विकास परिषद् में प्रधानमंत्री, नीति आयोग (योजना आयोग) के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री संघशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा भारत सरकार के प्रमुख विभागों के कुछ मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकासपरिषद् के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
(1) राष्ट्रीय योजनाओं की प्रगति पर समय-समय पर विचार करना।
(ii) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने की आर्थिक एवं सामाजिक तथा सामाजिक नीतियों संबंधी विषयों पर विचार करना।
(iii) राष्ट्रीय योजनाओं के निर्धारण एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना।
(iv) राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण के लिए तथा इसके साधनों के निर्धारण के लिए पथ प्रदर्शक सूत्र निश्चित करना।
(v) नीति आयोग (योजना आयोग) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना।
(vi) समय-समय पर योजना के कार्य की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना में प्रतिपादित उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।
35. ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें।
Ans – बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था है। राज्य सरकार लगभग 7800 की ग्रामीण आबादी पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना कर सकती है। एक ग्राम पंचायत में एक गाँव या कई गाँव हो सकते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की सबसे नीचला एवं महत्त्वपूर्ण स्तर है। स्थानीय समस्याओं के समाधान एवं जनता के कल्याण में ग्राम पंचायत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम पंचायत के अधीन 29 महत्त्वपूर्ण विषय रखे गए हैं जिससे संबंधित कार्य ग्राम पंचायत को करने पड़ते हैं। ग्राम पंचायत के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं-ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना और वार्षिक वजट, सार्वजनिक सम्पति पर से अवैध कब्जा हटाना एवं सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना आदि ग्राम पंचायत के कार्यों के अन्तर्गत आते हैं।
ग्राम पंचायत को उपयुक्त कार्यों के अलावे भी कार्य करने पड़ते हैं जैसे-कृषि एवं बागवानी का विकास करना, पेयजल की व्यवस्था करना, सड़क, भवन, पुलिया और नाली आदि का निर्माण करना, गलियों एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना आदि। प्राथमिक, माध्यमिक, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा का विकास करना, बाजार, मेले, शौचालय आदि की व्यवस्था करना, धर्मशाला, छात्रावास एवं कसाईखाना आदि का निर्माण करना तथा जनवितरण प्रणाली पर नियंत्रण रखना आदि प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत को करने पड़ते हैं।
36. संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है ?
Ans – संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 ई० को हुई थी। इस संस्था का मुख्य कार्यालय न्यूयार्क अमेरिका में है।
उद्देश्य
(i) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखना।
(ii) भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना।
(iii) आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना।
(iv) ऊपर दिये गये हितों की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की कार्यवाही में तालमेल करना।
37. बिहार के संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें।
Ans – 1974 से 1980 का भारतीय इतिहास लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जायेगा। भारत में 1970 के दशक का प्रारंभ एकदलीय वर्चस्व की पराकाष्ठा के रूप में हुआ। “इंदिरा इज इंडिया” का नारा दिया जाने लगा। स्वाभाविक था कि सत्ता का दुरुपयोग होने लगा। 18 मार्च, 1974 को बिहार में इसी सत्ता दुरुपयोग के विरोध में छात्र आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए जयप्रकाश नारायण आगे आये। 5 जून, 1974 को गाँधी मैदान पटना की महती सभा में उन्होंने ‘संपूर्ण क्रांति’ का आह्वान किया। उनकी मान्यता थी कि लोकतंत्र पटरी से उतर चुकी है। जिन मूल्यों एवं आदशों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई वे भुलाये जा रहे हैं। शक्तियों का दुरुपयोग आम बात हो गई है। सत्ता का केन्द्रीकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री की भूमिका तानाशाह की हो गई है। संसद भी गूँगी हो गई है क्योंकि विपक्ष कमजोर है।
इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का अर्थ बतलाया ‘व्यवस्था में आमूल परिवर्तन- राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन।
उन्होंने इसे आजादी की दूसरी लड़ाई की संज्ञा दी। आंदोलन चलता रहा इसका दायरा बिहार से बाहर निकलकर संपूर्ण भारत तक फैल गया। संपूर्ण क्रांति के दूरगामी प्रभावों को देखा जा सकता है। भारत में पहली बार द्विदलीय स्थिति की संभावना उभरी। सभी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, संविधान की भावना का आदर, न्यायपालिका की स्वायत्तता आदि के मामले में पटरी से हटी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया।
ऐसा लगने लगा कि कुछ दिनों में सचमुच संपूर्ण क्रांति का सपना साकार हो जायेगा। किन्तु राजनीतिक कारणों से ऐसा हो नहीं पाया। ढाई वर्षों के बाद ही जनता पार्टी में फूट हो गई। जिसका लाभ कांग्रेस को मिला और वह पुनः सत्ता में 1980 में वापस आ गई। जयप्रकाश नारायण काफी बीमारी के कारण सत्ता को सही दिशा निर्देश नहीं दे सकते थे। जयप्रकाश नारायण के अनुयायी भी सत्ता के लोभ में मूल्यों एवं आदशों को भूलने लगे।
इस प्रकार संपूर्ण क्रांति अपने लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं कर सका, किन्तु यह दिखला दिया कि जनतंत्र सतत् जागरूकता की स्थिति में ही काम कर सकता है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी उम्मीद बना दिया कि जब कभी लोक मुद्दे को लेकर राजनीतिक नेतृत्व आगे बढ़ेगा, लोग उनके साथ होंगे। हाल में अन्ना हजारे के जन लोकपाल के मुद्दे पर उपजे जन समर्थन को इसी रूप में देखा जा सकता है।
38. सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है ?
Ans – जून, 2005 से देश के सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के तहत देश का कोई भी नागरिक सरकार से वांछित सूचना की माँग कर सकता है और सरकार को निर्धारित सूचना देनी पड़ती है। सूचना के अधिकार का यह आंदोलन जनआंदोलन की सफलता का सुंदर आंदोलन है। सूचना के अधिकार के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
(i) नागरिकों को अपने कर्त्तव्य के प्रति सशक्त बनाना। एक नागरिक होने के नाते उन्हें देश के प्रति क्या कर्त्तव्य है। एक समाज के प्रति क्या कर्त्तव्य है। एक परिवार के प्रति क्या कर्त्तव्य है आदि। इन्हीं सब कायों के
(i) नागरिकों को अपने कर्त्तव्य के प्रति सशक्त बनाना। एक नागरिक होने के नाते उन्हें देश के प्रति क्या कर्त्तव्य है। एक समाज के प्रति क्या कर्त्तव्य है। एक परिवार के प्रति क्या कर्त्तव्य है आदि। इन्हीं सब कार्यों के प्रति नागरिकों को शसक्त रहने के लिए सूचना अधिकार आंदोलन चला।
(ii) सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाना इस आंदोलन की मुख्य उद्देश्य रहा है। इस आंदोलन की मुख्य मांग थी। सरकार जो कार्य कर रही है या सरकार की जो कार्य है उसमें पारदर्शिता लाना। सरकार के कार्यों एवं उसके निष्पादन के तौर तरीके तथा उन पर आनेवाले खर्च का पूरा व्योरा सूचना पट्ट या समाचार के माध्यम से लोगों को बताया जाता है।
(iii) सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही को यह आंदोलन मजबूत करता है। सरकार जो भी कार्य करती है या निर्णय लेती है, उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि बातों का प्रभाव इन आंदोलन का रहा है।
‘(iv) इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा है- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सरकारी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना। क्योंकि सूचना के अधिकार कानून बन जाने के बाद कोई भी व्यक्ति सरकार या सरकारी संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मांग सकता है। इसलिए सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार को समाप्त करना।
यदि आपको यह मॉडल पेपर पसंद आया हो तो इसे लाइक , कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ” धन्यवाद “
Important Links
| My Official Website | Visit Now |
|---|---|
| Youtube Channel | Click Here |
| Whatsapp Channel | Click Here |
| Telegram Channel | Click Here |
| Instagram Id | Click Here |